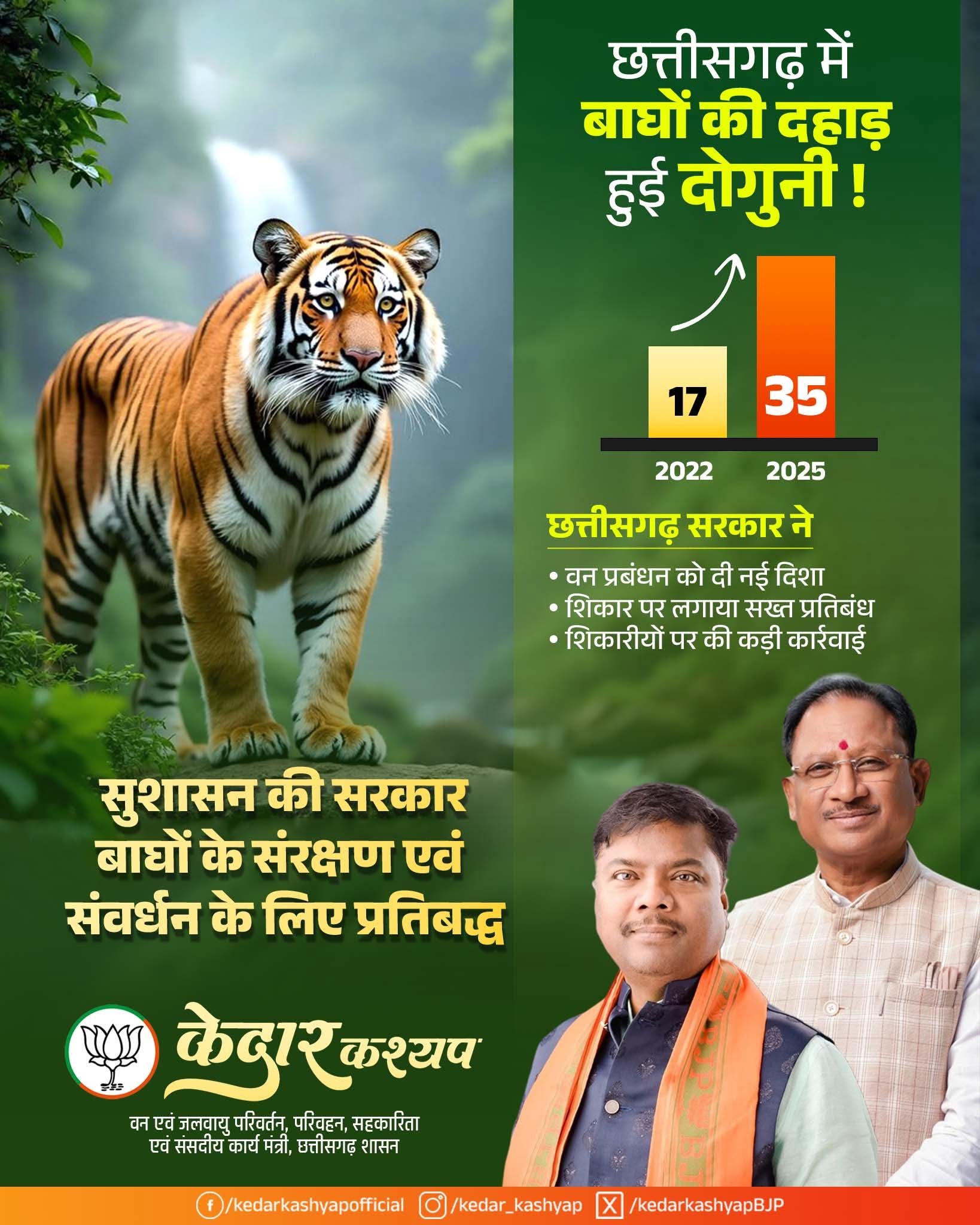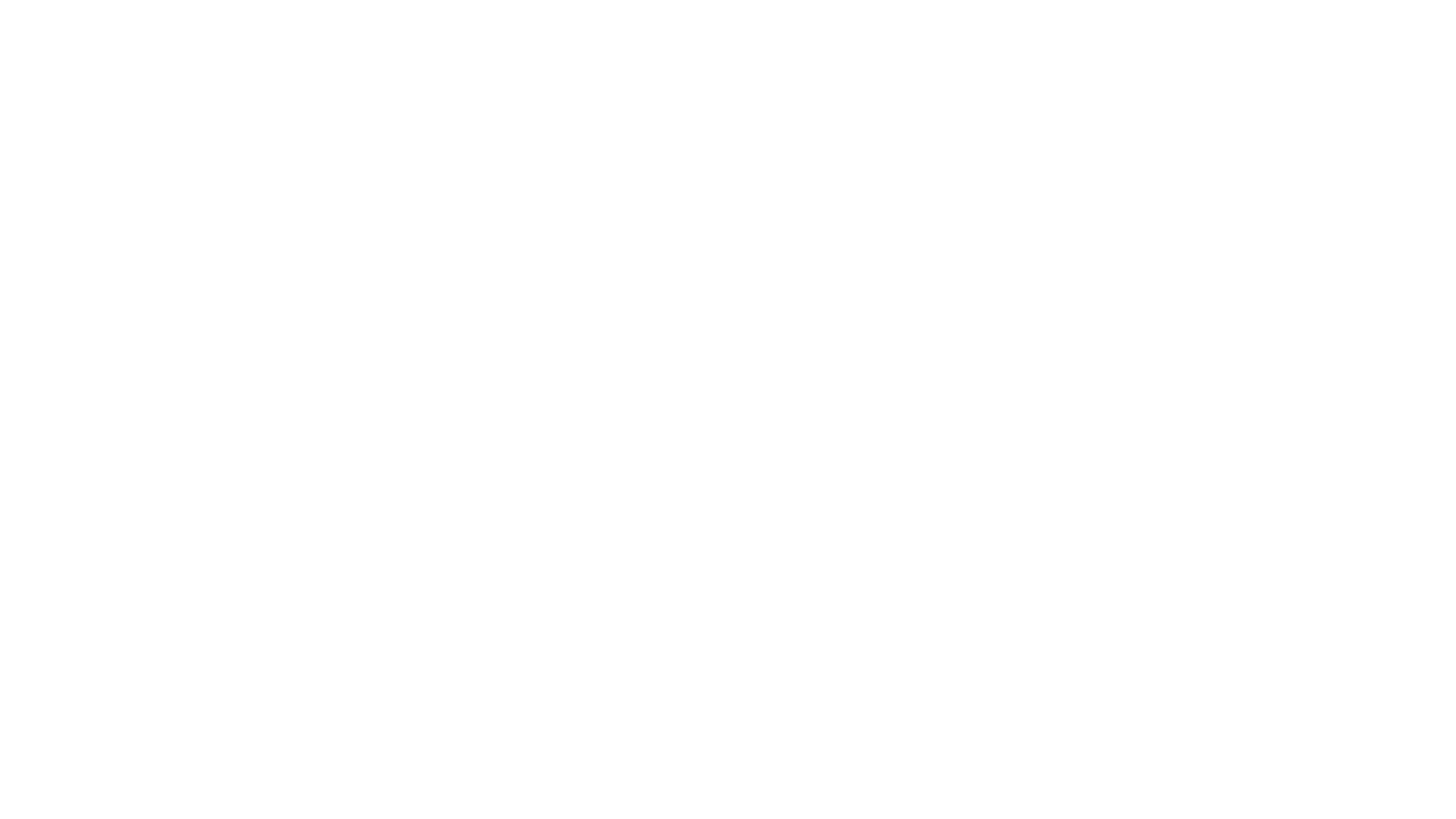मनीष कुंजाम पिछले चार दशकों से राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बस्तर में सक्रिय हैं. छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पहले वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की ओर से दो बार (1990-98) विधायक रह चुके हैं. जब सुकमा जिले के कलेक्टर का 2012 में अपहरण हुआ, उनकी रिहाई में कुंजाम की अहम भूमिका रही थी.
माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत शुरू हुए विवादास्पद ‘सलवा जुडुम’ अभियान के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाले लोगों में कुंजाम भी शामिल थे. तब सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में इस मामले में फैसला देते वक्त कहा था कि आम लोगों के हाथों में शस्त्र देकर उन्हें माओवादियों के खिलाफ लड़ाना अवैध है, और राज्य सरकार तुरंत इस अभियान को रोक दे.
कुंजाम अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं. हाल ही में उन्होंने भाकपा के सभी पदों से इस्तीफा देकर दिसंबर 2024 में अपनी अलग पार्टी ‘बस्तरिया राज मोर्चा’ का गठन किया है.
पिछले एक साल में केंद्र सरकार ने माओवाद विरोधी अभियान तेज़ किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक माओवाद खत्म करने की घोषणा की है. कुछ दिन पहले ही माओवादी पार्टी के महासचिव बसवाराजू सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए. मनीष कुंजाम इस बातचीत में आदिवासी क्षेत्र में शांति की संभावना, सरकार और माओवादियों की भूमिका और विकास प्रक्रिया के बारे में अपना पक्ष रखते हैं.
आपने 2013 में सरकार और माओवादियों के बीच शांतिवार्ता करवाने की कोशिश की थी. तब कोई बातचीत नहीं हुई. मगर अब माओवादी पार्टी लगातार सरकार से युद्धविराम और बातचीत की अपील कर रही है. आपके पिछले प्रयासों का अनुभव क्या रहा था, और क्या इस बार आप शांतिवार्ता की कोई संभावना देखते हैं?
कुंजाम: अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की ओर से हमने मार्च 2013 में पंद्रह दिन की पदयात्रा निकाली थी और माओवादियों और सरकार से शांति के लिए बातचीत करने की अपील की थी. पदयात्रा के दौरान दंतेवाड़ा, सुकमा और जगदलपुर में तीन बड़ी सभाएं हुईं. इसे स्थानीय लोगों का भी भरपूर समर्थन मिला. लेकिन उस समय माओवादियों ने मुझ पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाया था कि पदयात्रा करने वाले शांति की बात करके ‘जनवादी क्रांति’ को कमजोर कर रहे हैं.
उस समय माओवादी बहुत शक्तिशाली थे. माहौल भी ऐसा था कि अगर वे कुछ मांग करते, तो सरकार उन्हें मानने के लिए मजबूर हो जाती. लेकिन तब उन्होंने हमारी अपील नहीं सुनी. अब माओवादी शांतिवार्ता का प्रस्ताव रख रहे हैं. यह उनकी मजबूरी है. वे थक चुके हैं और जनता का समर्थन भी उन्हें पहले की तरह नहीं मिल रहा. इसके अलावा पूरे बस्तर में हर जगह सुरक्षा बलों के कैंप लगे हुए हैं.
जो भी हो, मुझे लगता है कि शांतिवार्ता तो होनी ही चाहिए. माओवादी आंदोलन सिर्फ बस्तर तक सीमित नहीं है. वह अन्य जगहों पर भी आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं. बस्तर का बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से भरा हुआ है. जब सुरक्षा बलों ने यहां के कर्रेगुट्टा पहाड़ियों में कार्रवाई की (मई 2025 में बीजापुर के पास इन पहाड़ियों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में तीस से अधिक माओवादियों को मार गिराया था), तो जवानों को रास्ता ढूंढने में बीस दिन लग गए थे.
दूरदराज के इलाकों में ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं, वहां हथियारों की फैक्ट्रियां हैं, हथियार छिपाकर रखे हुए हैं. इसलिए केवल कुछ समय के लिए माओवादियों के खिलाफ ताकत लगाकर कार्रवाई करने से शांति स्थापित नहीं होगी. अगर माओवादी नेता खुद ही अपने हथियार डाल देंगे, तब स्थायी शांति स्थापित होगी और सशस्त्र गतिविधियों की कोई संभावना नहीं रहेगी. इसलिए उनसे बात करना जरूरी है, ताकि हिंसा फिर न भड़के और निर्दोष लोगों की जान न जाएं.
लेकिन सरकार बातचीत के बजाय सशस्त्र कार्रवाई के द्वारा ही माओवाद को खत्म करना चाह रही है.
सिर्फ माओवादी ही नहीं, बल्कि कोई भी व्यक्ति अगर पहले गुनहगार था और संविधान नहीं मानता था, और वह अब हथियार डालने और संविधान के दायरे में बात करने को तैयार है, तो लोकतांत्रिक सरकार को उससे बात करनी चाहिए. सरकार पूर्वोत्तर भारत में और कश्मीर में उग्रवादियों से बात करती है, तो फिर माओवादियों से चर्चा करने में कौन-सी दिक्कत है. ‘आत्मसमर्पण करो या मरो’, सरकार का ये रुख गलत है.
मुझे ऐसा लगता है कि सरकार खुद ही माओवाद को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहती. माओवादी गतिविधियां छिटपुट स्तर पर जारी रहती है, तो लोकतांत्रिक, संवैधानिक और अहिंसक आंदोलनों को कुचलने के लिए इन आंदोलनों मे शामिल कार्यकर्ताओं को ‘नक्सली’ कहकर जेल में डालने के लिए और गैरकानूनी कतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) जैसे सख्त कानूनों का इस्तेमाल करने के लिए सरकार को बहाना मिल जाता है.
इसके पीछे कॉरपोरेट कंपनियों का दबाव भी हो सकता है. झारखंड में कंपनियों के समर्थन से ऐसी कुछ ताकतों को बनाए रखा गया है. बस्तर में भी बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों को हड़पना, ये इसके पीछे का मकसद है. इन संसाधनों की लूट का संवैधानिक तरीकों से विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं पर माओवाद के बहाने कार्रवाई किया जाना धोखा है. अगर नक्सलवाद खत्म हो जाए, तो यहां इतने बड़े पैमाने पर बनाए गए पुलिस कैंप्स का कोई बहाना नहीं रहेगा.

संसाधनों का मुद्दा विकास की अवधारणा से जुड़ा हुआ है. जब तक हमारी विकास की मुख्यधारा की अवधारणा कायम है, तब तक उसके लिए कोयला, यूरेनियम और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता लगती रहेगी, जो बस्तर जैसे आदिवासी इलाकों में भारी मात्रा में है. ऐसे में माओवाद हो या न हो, हिंसा हो या न हो, स्थानीय आदिवासी इलाकों के शोषण की संभावना बनी रहती है. इसके बारे में क्या किया जा सकता है?
बस्तर का यह हिस्सा पांचवीं अनुसूची में आता है. यहां ‘पेसा कानून’ (पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों मे विस्तार अधिनियम, 1996) लागू है. इसके अनुसार, ग्राम सभाओं को गौण खनिज और लघु वनोपज के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है. इसके अलावा राष्ट्रीयकृत खनिजों के मामले में भी स्थानीय ग्राम सभाओं की सहमति लेनी अनिवार्य है. इस विकास में आदिवासियों की हिस्सेदारी होनी चाहिए.
छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, ओडिशा हो, मध्य प्रदेश हो, या कहीं और, ये सभी खदानें और संसाधन मुख्य रूप से आदिवासी इलाकों में हैं. जहां खनन हो रहा है, वहां के आदिवासियों की स्थिति क्या है? उनको इस विकास का कुछ लाभ मिला है? इन खनन परियोजनाओं से कंपनियों को जो मुनाफा होता है, उसका आधा हिस्सा आदिवासियों को देने में क्या दिक्कत है? इस विकास से सिर्फ सरकार, पूंजीपति और कंपनियां मालामाल हो रहे हैं. आदिवासियों ने देश के विकास के लिए बलिदान दिया, इतने संसाधन दिए, बदले में आदिवासियों को क्या मिला? अभी तो सिर्फ पंद्रह-बीस उद्योगपतियों के फायदे के लिए विकास हो रहा है.
हमारे यहां गांव को लेकर एक सामाजिक सोच है. हर गांव अपने आप में एक स्वतंत्र कहानी है, 1996 के ‘पेसा कानून’ ने उसको मान्यता दी. उससे ग्रामसभा को स्वायत्त संस्था का दर्जा मिला. इसलिए यहां के विकास से जुड़े फैसलों में गांव को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. लेकिन हकीकत में गांव की विकास योजना बनाने में ग्रामीणों की भागीदारी नहीं होती.
हम कोई अलग मांग नहीं कर रहे, हम सिर्फ कानून को लागू करने की मांग कर रहे हैं.
दिल्ली या रायपुर में बैठकर बनाई गई विकास की योजना यहां थोप दें, तो कैसे चलेगा! प्रशासनिक स्तर पर आप ग्रामीणों को सलाह जरूर दें, लेकिन ऊपर सें योजना न थोपें, इतना ही हमारा कहना है.
संसाधनों के दोहन के खिलाफ आप अहिंसक, संवैधानिक तरीकों से प्रतिरोध करते रहे हैं. टाटा, एस्सार आदि कंपनियों के खिलाफ आपकी लड़ाई सफल रही है. सलवा जुडुम के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी सफल रही. लेकिन डेढ़ साल पहले मध्य भारत में कई आदिवासी इलाकों में खदानों के खिलाफ संवैधानिक विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया में कोई जगह नहीं मिली. गढ़चिरोली में सूरजगढ़ खदान के खिलाफ दो सौ दिनों से ज्यादा चले प्रदर्शन पर नवंबर 2023 में एक दिन अचानक कार्रवाई कर आंदोलन खत्म कर दिया गया. यह सच है कि इन विरोध प्रदर्शनों का माओवादियों ने समर्थन किया था; लेकिन इसमें शामिल लोग लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात रख रहे थे. क्या सरकार को उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी?
अगर माओवादियों का किसी भी विरोध प्रदर्शन से अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ाव हो, तो ऐसे प्रदर्शनों को नजरअंदाज करने का और उनकी मांगों के प्रति उदासीन रहने का बहाना सरकार को मिल जाता है. इसलिए सशस्त्र संघर्ष को बंद कर अहिंसक प्रतिरोध करने की जरूरत है. गांधीजी बिना हथियार के सरकार को सवाल पूछते थे. हमने हाल ही में विरोध प्रदर्शन कर बैलाडिला में खदान नंबर 13 का अडानी कंपनी को दिया हुआ ठेका रद्द करवाया.
(राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम ने संयुक्त रूप से बैलाडिला पहाड़ियों में परियोजना बनाई है. इसके खनन का ठेका दिसंबर 2018 में अडानी समूह को दिया गया था. लेकिन उस पहाड़ी पर स्थानीय देवता नंदराज का मंदिर है और इस खनन के लिए ग्रामसभा की फर्जी अनुमति ली गई थी, ऐसे भी आरोप लगे. इसके बाद लोगों ने एकजुट होकर इस खदान के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया और खनन रद्द करना पड़ा.)

आप कई साल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे. पिछले चुनाव में चुनाव चिह्न न मिलने पर पार्टी नेतृत्व से विवाद के बाद आपने पार्टी छोड़ दी. किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी का समग्र मानवी व्यवस्था के बारे में एक वैचारिक दृष्टिकोण है. अब ‘बस्तरिया राज मोर्चा’ पार्टी अस्तित्व में आई है. क्या यह कहा जा सकता है कि आपकी वैचारिक यात्रा साम्यवाद/मार्क्सवाद जैसे दर्शनों, वर्गीय दृष्टिकोण से अब स्थानीय दृष्टिकोण, स्थानीय संस्कृति की ओर चली गई है?
छात्र जीवन में मार्क्स-लेनिन से प्रभावित हुआ. वह विचार तो हमेशा साथ रहेगा. यह विचार गरीबों के पक्ष में है. यहां तो मुख्य रूप से स्थानीय लोग ही गरीब हैं. बाहरी लोग, ठेकेदार और व्यापारी जैसे गैर-बस्तरिया लोगों का संसाधन पर कब्जा है. ऐसा लगता है कि वे यहां शोषण करने आए हैं.
बस्तर में इस तरह के शोषण के खिलाफ लड़ाई का इतिहास रहा है. 1910 में यहां ‘भूमकाल विद्रोह’ हुआ था. उस समय अंग्रेजों ने यहां के जंगलों को आरक्षित करने की और के वनोपज का उपयोग कुछ कंपनियों को करने की अनुमति देने की कोशिश की. फिर यहां की स्थानीय जनजातियों ने एकजुट होकर ‘जल-जंगल-ज़मीन’ के मुद्दे पर विद्रोह कर दिया. हम भी वही कर रहे हैं. हम अहिंसक लोकतांत्रिक तरीकों से ऐसा कर रहे हैं.
लेकिन आपने पार्टी के नाम में बस्तर स्थान का इस्तेमाल किया है. यह स्थानीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला नाम है. क्या आपकी राजनीति का रास्ता बदल गया है?
रास्ता यही था. अब यह कहा जा सकता है कि और स्पष्टता आई है.
बस्तर को स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया जाए, ऐसी भी मांग आपने की है.
यह हमारी पुरानी मांग है. कम्युनिस्ट पार्टी ने 1967-68 के दौरान जगदलपुर में हुई किसान सभा की बैठक में बस्तर को छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्तता देनी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव पारित किया था. 1995-96 के दौरान भी छठी अनुसूची लागू करने के लिए यहां लंबा आंदोलन चला था. (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) और (2) मे पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के प्रावधान हैं.)
पांचवीं अनुसूची पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर देश के बाकी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लागू होती है; वहां ग्राम सभाओं को अन्य कुछ अधिकारों के साथ ही अपने क्षेत्रों में संसाधनों के बारे में निर्णय लेने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त है. छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में लागू होती है, जहां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अलग से विशेष अधिकार प्राप्त है. बस्तर पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है).
दरअसल, ‘पेसा कानून’ में ही कहा गया है कि पांचवीं अनुसूची में शामिल जिला पंचायतों को छठी अनुसूची के क्षेत्रों की जिला पंचायतों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए. मतलब कानून में ही स्वायत्तता का विस्तार अपेक्षित है.

आपने स्वायत्तता की बात की, बाहरी लोगों और स्थानीय लोगों का जिक्र किया. लेकिन लोग किसी न किसी कारण से यहां से वहां आते-जाते रहेंगे. इन बाहरी लोगों का स्थान क्या है? उनकी यहां क्या भूमिका होनी चाहिए?
यह हम सबका देश है. इसलिए यहां सभी आएं. लेकिन आदिवासी इलाकों की आदिवासीयत जीवित रखनी चाहिए. यहां का विकास आदिवासियों की दृष्टि से होना चाहिए. बाहरी लोग यहां आकर सिर्फ ज़मीन खरीद लेंगे और बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसा कैसे चलेगा!
जो लोग बाहर से आए हैं, उन्हें स्थानीय लोगों के प्रति हमदर्दी और संवेदनशीलता रखनी चाहिए.
इतने दशकों से इस पूरे इलाकों मे रह रहे लोगों ने खूनखराबा देखा है. चाहे जितनी भी शांति की बात कही जाए, युद्ध अभी भी जारी है. उसका सदमा लोगों के भीतर निरंतर है. इसका क्या समाधान हो सकता है?
इन सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक तरीकों से चल रहे संघर्ष और तेज किए जाने चाहिए. नागरी सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, रोजगार देना चाहिए. साथ ही ‘जल-जंगल-ज़मीन’ का संघर्ष भी जारी रहना चाहिए. आदिवासियों का अस्तित्व ही ज़मीन और जंगल पर टिका हुआ है. आदिवासियों का विकास आदिवासी दृष्टि से होना चाहिए.
(अवधूत डोंगरे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित लेखक और अनुवादक हैं.)