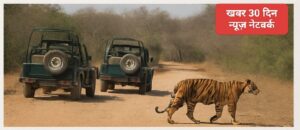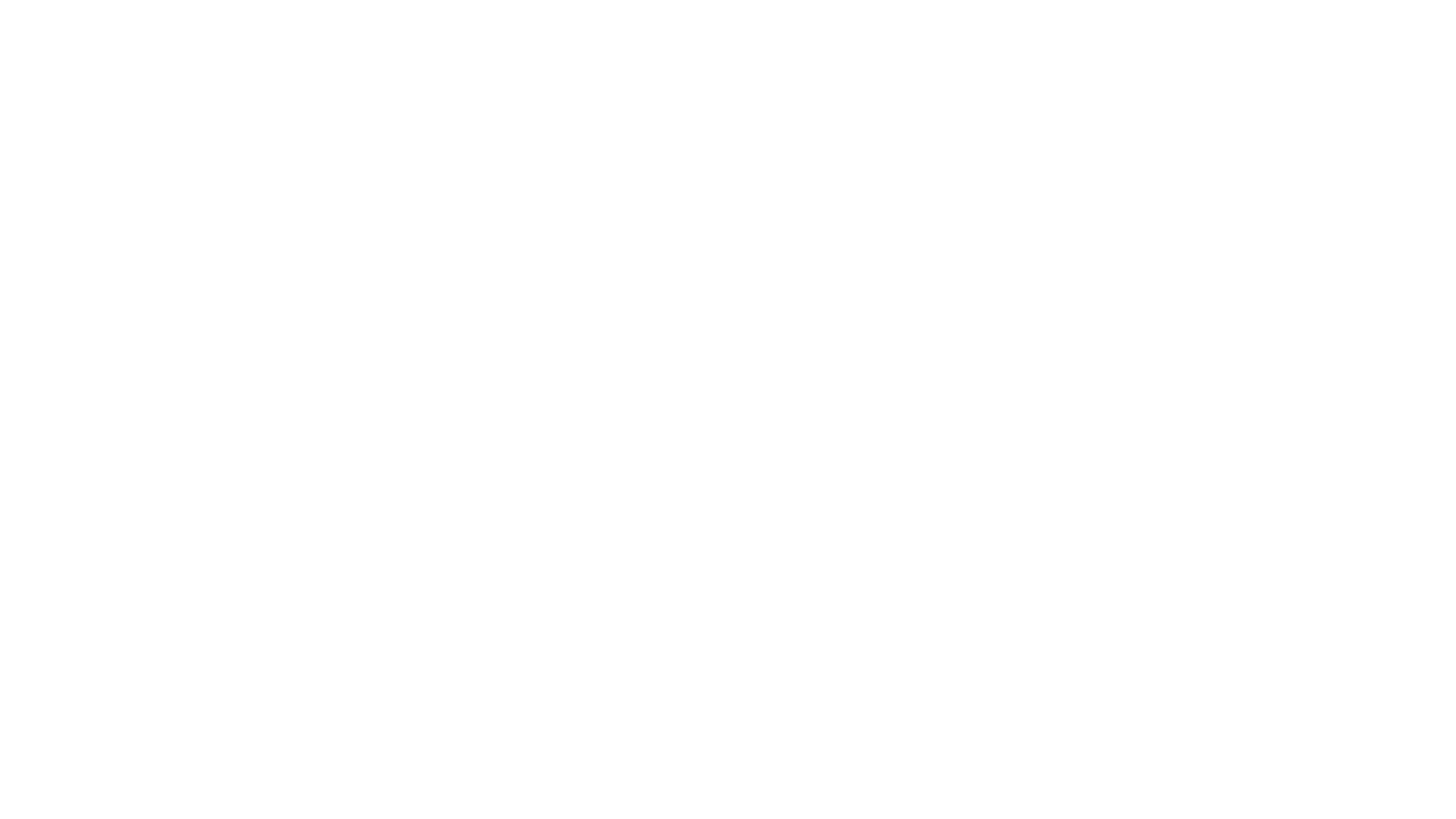खबर 30 दिन न्यूज़ नेटवर्क।अब्दुल सलाम क़ादरी। देश के कई हिस्सों में अप्रैल महीने से ही तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच चुका है। हीटवेव की चेतावनियाँ लगातार दी जा रही हैं और गर्मी का असर सिर्फ शरीर पर नहीं, खेती, जल संकट और बिजली की मांग पर भी दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि आखिर हर साल गर्मी क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे केवल मौसम नहीं, बल्कि इंसानी गतिविधियाँ, विकास मॉडल और वैश्विक जलवायु संकट की बड़ी भूमिका है।
1. जलवायु परिवर्तन: ग्लोबल वार्मिंग का लोकल असर
जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति के बाद से अब तक करीब 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है।
इसका सीधा असर इन बातों पर पड़ा है:
- गर्मियों की शुरुआत पहले हो रही है।
- हीटवेव की अवधि लंबी हो रही है।
- रातों का तापमान भी सामान्य से ज्यादा है, जिससे राहत नहीं मिलती।
भारत जैसे ट्रॉपिकल देश में इसका असर और गंभीर होता है क्योंकि पहले से ही यहां गर्मी ज्यादा होती है।
2. शहरीकरण और हरियाली का खत्म होना
स्थानीय स्तर पर भी कई कारण गर्मी को बढ़ा रहे हैं:
- पेड़ों की कटाई: सड़कों, इमारतों और परियोजनाओं के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे ठंडी हवाओं का रास्ता बंद हो जाता है।
- कंक्रीट का जंगल: शहरों में इमारतें, सीमेंटेड सड़कें और गाड़ियों की भरमार गर्मी को सोख लेती है, जिसे रात में धीरे-धीरे छोड़ा जाता है। इसे “Urban Heat Island Effect” कहते हैं।
- जल स्रोतों की कमी: पोखर, तालाब और नदियाँ सूखती जा रही हैं, जो पहले आसपास के इलाके का तापमान संतुलित रखने में मदद करती थीं।
3. बढ़ते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन
कोयले से चलने वाले बिजलीघर, पेट्रोल-डीज़ल से चलने वाले वाहन, और खेतों में रसायनों का इस्तेमाल – ये सभी मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें छोड़ते हैं। ये गैसें धरती की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देतीं, जिससे वातावरण गर्म होता है।
4. हीटवेव का सामाजिक असर
- स्वास्थ्य पर प्रभाव: हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और स्किन डिजीज़ के मामले बढ़ते हैं।
- कामकाजी वर्ग पर असर: दिहाड़ी मजदूर, किसान और रेहड़ी-पटरी वाले सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उन्हें खुले में काम करना पड़ता है।
- बिजली और पानी की मांग: बिजली कटौती और पानी की किल्लत से स्थिति और गंभीर हो जाती है।
5. समाधान की राह: क्या किया जा सकता है?
- स्थानीय उपाय: पेड़ लगाना, जल स्रोतों को बचाना, और छाया वाले सार्वजनिक स्थान बनाना।
- सरकारी नीतियाँ: शहरों की योजना में जलवायु के अनुकूल डिजाइन शामिल करना, रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देना।
- व्यक्तिगत प्रयास: एयर कंडीशनर की जगह कूलर या नैचुरल वेंटिलेशन, छतों पर ग्रीन रूफ या सफेद पेंट, पानी की बचत जैसे छोटे-छोटे कदम।
निष्कर्ष:
गर्मी का बढ़ना अब केवल मौसम का उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि एक स्थायी संकट बन चुका है। इसे रोकने के लिए हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर ठोस कदम उठाने होंगे। वरना आने वाले सालों में 50 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी एक आम बात हो जाएगी।