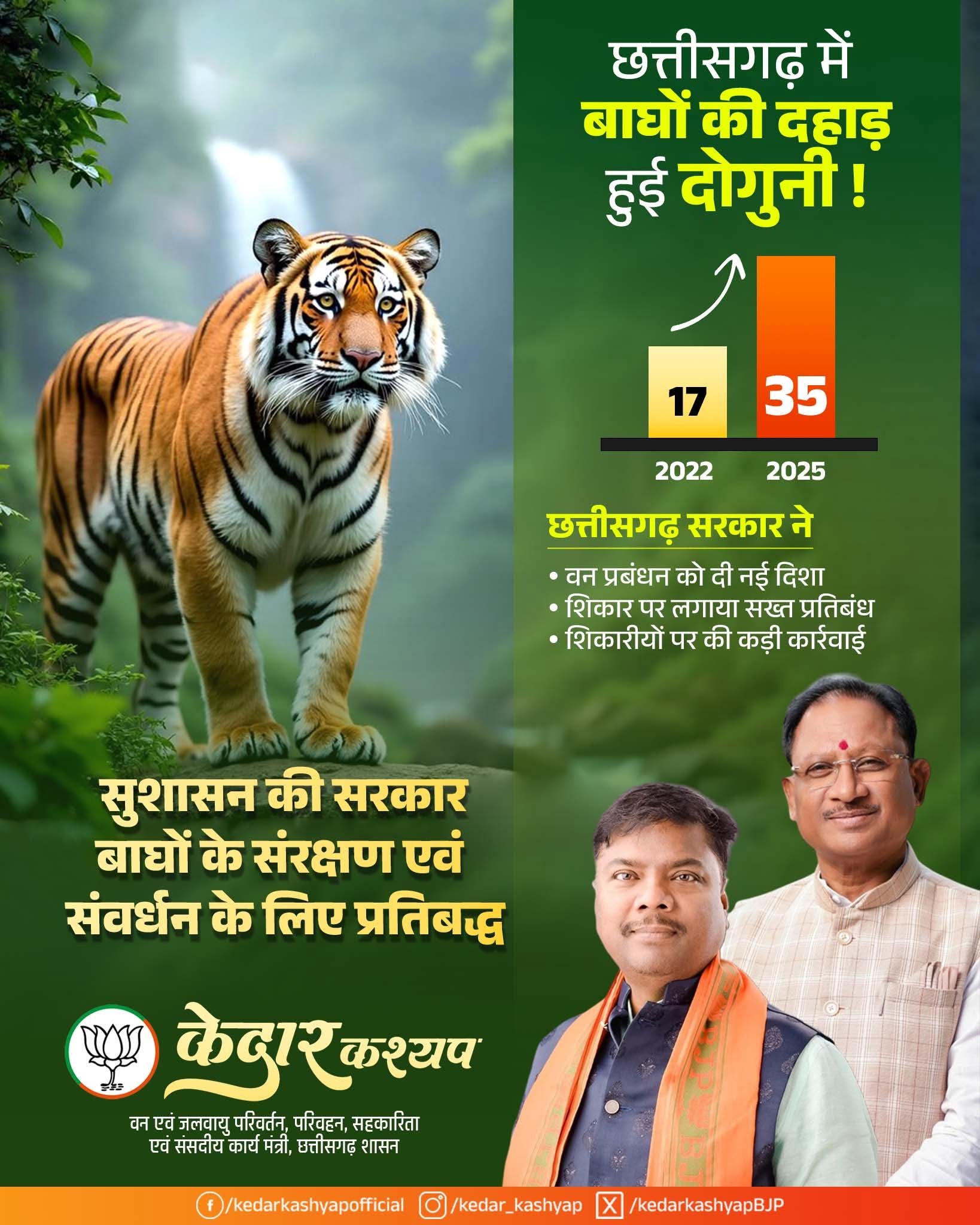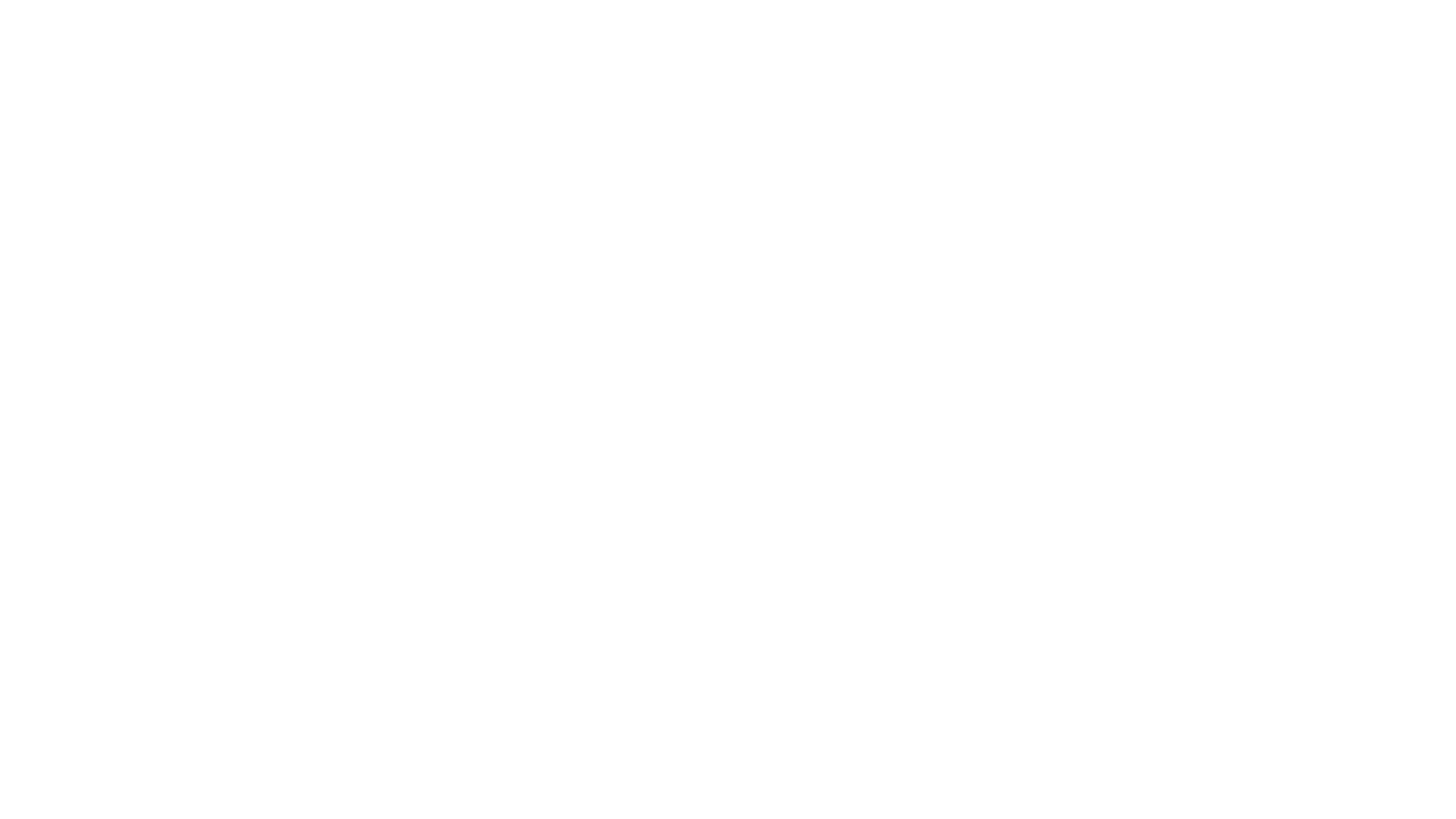लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर शोर इतना बढ़ गया है कि ‘ध्वनि निषेध क्षेत्र’ भी तेज़ आवाज़ों के नीचे दबते जा रहे हैं. अस्पताल, कॉलेज और सार्वजनिक संस्थानों के बाहर तेज़ हॉर्न और लाउडस्पीकर दिन-रात गूंजते हैं. ‘ध्वनि निषेध क्षेत्र’ वे इलाके हैं जहां ध्वनि सीमा तय होती है, ताकि नागरिकों को शांति मिल सके, जैसे स्कूल, अस्पताल या न्यायालय.
लेकिन लखनऊ के 10 रियल टाइम नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 3 प्रमुख ‘ध्वनि निषेध क्षेत्रों’ में शोर का स्तर डब्ल्यूएचओ की सीमा 50 dB(A) को पार करते हुए 65–70 dB(A) तक पहुंच चुका है. यह न सिर्फ़ तकनीकी विफलता है, बल्कि नीति और निगरानी ढांचे पर भी सवाल खड़ा करता है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2011 में शुरू की गई ‘नेशनल एंबिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क’ (एनएएनएमएन) योजना का उद्देश्य देश के प्रमुख शहरों में शहरी शोर स्तर की नियमित निगरानी सुनिश्चित करना था. वर्ष 2021–23 में इस नेटवर्क का विस्तार 7 से बढ़ाकर अब 8 शहरों तक कर दिया गया है, जहां कुल 75 रियल-टाइम नॉइस मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं.
हालांकि, लखनऊ जैसे शहरों में यह प्रणाली केवल एक डैशबोर्डa तक सिमटकर रह गई है. न तो जन-जागरूकता बढ़ी है, और न ही कोई ठोस नीतिगत कार्रवाई शुरू हुई है. जब इन तीन क्षेत्रों में वास्तविक शोर स्तर का मूल्यांकन किया गया, तो स्पष्ट हो गया कि नेटवर्क अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा है क्योंकि ध्वनि स्तर अब भी मानकों से काफी अधिक है.
तकनीकी चूक या रणनीतिक अनदेखी?
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) की तकनीकी गाइडलाइंस कहती हैं कि मॉनिटरिंग सेंसर की ऊंचाई कम से कम 4 मीटर होनी चाहिए और किसी भी परावर्तक सतह से 3 से 5 मीटर दूर लगाया जाना चाहिए. अगर यह संभव न हो, तो आंकड़ों में -3 dB का सुधार करना आवश्यक होता है.
लेकिन लखनऊ में कई सेंसर इन मानकों का पालन नहीं करते, खासकर वे जो शांत क्षेत्रों में स्थापित हैं. एनएएनएमएन डैशबोर्ड पर इस संबंध में कोई स्पष्ट सूचना या समाधान नहीं दिखता.
ज़मीनी पड़ताल: लखनऊ के तीन प्रमुख ‘ध्वनि निषेध क्षेत्र’
1. एसजीपीजीआई हॉस्पिटल:
यहां का नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन भोजनालय की दीवार पर करीब 30 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया है और यह तीन दिशाओं से पेड़ों से घिरा हुआ है. इससे निगरानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. जब वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और डॉक्टरों से बातचीत की गई, तो उन्होंने सवाल किया — यदि यह वाकई शांत क्षेत्र है, तो फिर इसका बोर्ड परिसर में क्यों नहीं लगाया गया?

2. राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल
यहां भी सेंसर सीपीसीबी के मापदंडों पर खरे नहीं उतरते. सेंसर लगभग 35 फीट ऊंचाई पर दो हिस्सों में लगाए गए हैं—एक तरफ मॉनिटरिंग यूनिट, दूसरी ओर सेंसर, और ठीक सामने एक घना पेड़. लोहिया अस्पताल में तैनात एक गार्ड ने बताया कि दिनभर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ आईसीयू तक पहुंचती है. इससे न सिर्फ मरीज़ परेशान होते हैं, बल्कि तीमारदार भी चिड़चिड़े हो जाते हैं.

3. आईटी कॉलेज:
यहां का मॉनिटरिंग स्टेशन तीन दिशाओं से खुला है, लेकिन एक ओर यह पूरी तरह दीवार से ढका हुआ है, जिससे इसके माप पर सवाल उठते हैं. तेज़ शोर का असर वहां पढ़ने वाली छात्राओं की पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है लेकिन इस पहलू पर कोई निगरानी या प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली.

विशेषज्ञ राय और अंतरराष्ट्रीय मानक
सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान-नीरी में कार्यरत ध्वनि प्रदूषण विशेषज्ञ सतीश के. लोखंडे बताते हैं कि ‘फ्री फील्ड कंडीशन’ में सेंसर को किसी भी परावर्तक सतह से कम से कम 1 मीटर दूर रखना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो -3 dB का सुधार करना चाहिए जैसा कि ISO 1996-2:2007 में वर्णित है.
सीपीसीबी की 2015 की गाइडलाइन के अनुसार, एनएएनएमएन सेंसर की ऊंचाई 4–6 मीटर के बीच होनी चाहिए. ऐसे में अगर सेंसर 30 फीट (9.144 मीटर) पर लगे हैं, तो यह तकनीकी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है.
आईआईटी–बीएचयू के डॉ. अखिलेश कुमार यादव बताते हैं कि सेंसर की ऊंचाई और स्थापना यदि मानकों के अनुरूप नहीं हो, तो मापे गए आंकड़े ग़लत हो सकते हैं. इससे न केवल नीति-निर्माण भ्रमित होता है, बल्कि पर्यावरणीय न्याय की दिशा में एक गंभीर चूक भी साबित हो सकता है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की इनवायरनमेंटल नॉइज़ गाइडलाइन्स फॉर द यूरोपियन रीजन, 2018 की रिपोर्ट दर्शाती है कि लगभग 1.5 मीटर ऊंचाई तक शोर की माप ही स्वास्थ्य पर पड़ते प्रभावों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है. ऊंचाई बढ़ने से परिवेशीय शोर के वास्तविक स्तर में गिरावट दिखती है, जो डेटा को कम विश्वसनीय बनाता है.
यूपीपीसीबी की प्रतिक्रिया और सीमाएं
केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड के पायलट प्रोजेक्ट से जुड़े एक वैज्ञानिक और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक वैज्ञानिक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सेंसर ऊंचाई पर इसीलिए लगाए गए ताकि चोरी या क्षति से बचाव हो सके. हालांकि, 16 और 24 अप्रैल को सीपीसीबी दिल्ली मुख्यालय के नॉइस डिवीजन से मेल द्वारा संपर्क करने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, जिससे यह साबित होता है कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भारी कमी है.
YHonk के सीईओ सत्येन इंजीनियर सवाल उठाते हैं कि जब संविधान हमें शांत माहौल में जीने का अधिकार देता है, तो फिर साइलेंस ज़ोन में शोर रोकने के लिए यह संस्था क्या कर रही है? क्या साइलेंस ज़ोन के संकेत भी लगाए गए हैं?
डेटा है, दिशा नहीं
शांत क्षेत्रों में शोर का स्तर 60–70 dB(A) तक है, जबकि अनुमेय सीमा 40–50 dB(A) है. लेकिन यह नहीं पता कि प्रशासन इन आंकड़ों का क्या उपयोग कर रहा है. न ही यह पता है कि नगर निगम या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है.
यूपीपीसीबी की वेबसाइट पर वर्ष 2025, जनवरी-जून के आंकड़े अपलोड नहीं किए गए हैं, और वार्षिक रिपोर्ट 2018–19 के बाद से उपलब्ध नहीं है. यह पारदर्शिता के दावों पर गंभीर सवाल उठाता है.
लखनऊ के ध्वनि निषेध क्षेत्रों में ‘शांति’ अब मिथक बन गई है. नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन केवल औपचारिक उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उनका डेटा ज़मीनी कार्रवाई में कोई बदलाव नहीं ला पा रहा.
(रोहन सिंह, डाउन टू अर्थ’–’सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट’ के फेलो हैं व पर्यावरण के मामलों, के साथ ही बाल अधिकारों पर केंद्रित लेखन करते हैं.)