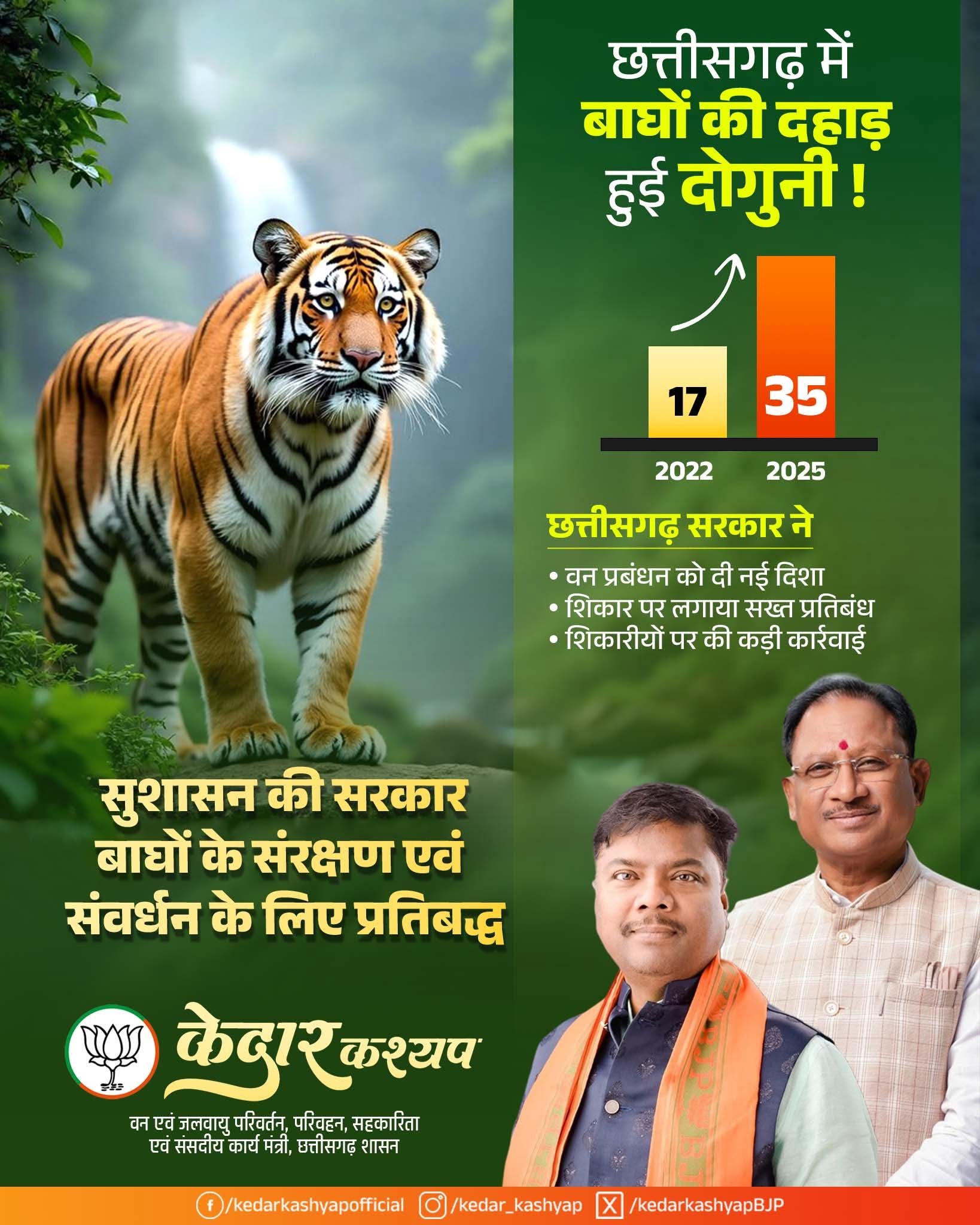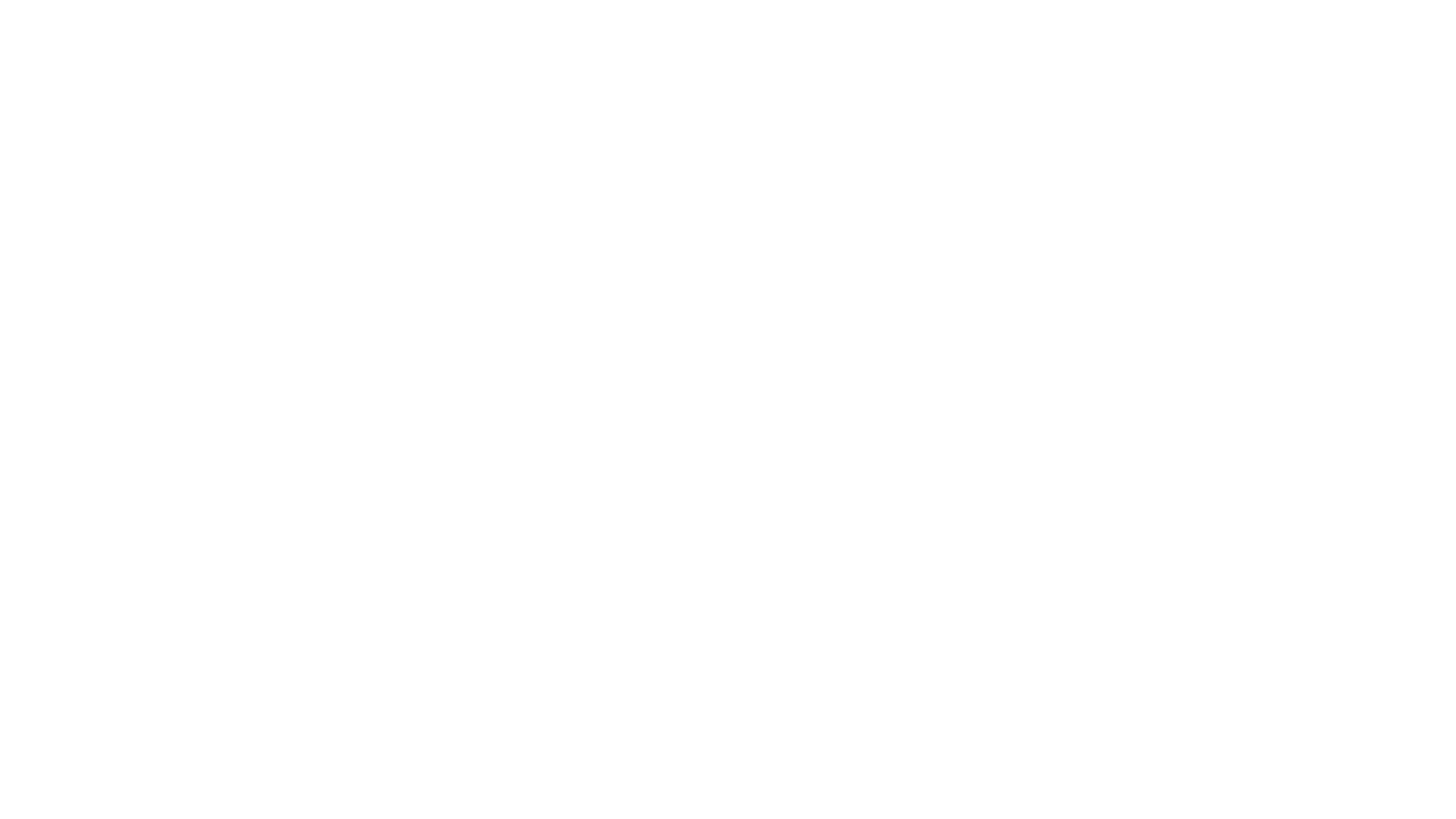पिछले दिनों मीडिया में छपी खबरों के अनुसार, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत खर्च पर कुछ पाबंदियांं लगाई हैं. 10 जून को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित खबर के अनुसार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए मनरेगा के तहत खर्च को अपने वार्षिक आवंटन के 60 प्रतिशत पर सीमित कर दिया है. सरकार का यह निर्णय मनरेगा की मूल अवधारणा के खिलाफ है.
मनरेगा की मूल अवधारणा की अवहेलना
मनरेगा मांग पर आधारित योजना है जिसमे कोई भी बेरोजगार काम मांग सकता है. मांग के आधार पर काम मनरेगा की मूल भावना है. यह काम मज़दूर वित्तीय वर्ष में किसी भी महीने में मांग सकता है. इसी अवधारणा के चलते मनरेगा को वित्त मंत्रालय के सरकारी खर्च को नियंत्रण करने के नियमों से बाहर रखा गया था.
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2017 में मासिक/त्रैमासिक व्यय योजना (MEP/QEP) को लागू किया था जिसका तथाकथित मक़सद मंत्रालयों को नकदी प्रवाह प्रबंधन और अनावश्यक उधारी से बचने में मदद करना था. अब तक मनरेगा को इसके दायरे से बाहर रखा गया क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय का तर्क था कि यह एक मांग आधारित योजना है, जिस पर खर्च की एक निश्चित सीमा तय करना व्यवहारिक नहीं है. लेकिन वित्त वर्ष 2025–26 की शुरुआत में, वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को निर्देश दिया है कि मनरेगा को भी MEP/QEP ढांचे के अंतर्गत रखा जाएगा.
केंद्र सरकार की नीति और ‘रोजगार के अधिकार’ पर हमला
हालांकि, भाजपानीत केंद्र सरकार के इस फैसले से किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह कोई इकलौता ऐसा फैसला नहीं है जो न केवल ग्रामीण भारत में रोजगार मुहैया करवाने वाले मनरेगा को कमजोर करेगा बल्कि इसके तहत ‘रोजगार के अधिकार’ के भी खिलाफ है. बजट में लगातार कटौती से लेकर भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर नित नई जटिलताएं पैदा करने वाली तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किये जाने वाले सभी कदम मनरेगा के मौलिक सिद्धांत को कमजोर करना ही है.
अगर उपरोक्त निर्णय लागू होता है तो इसका मतलब है कि इस वर्ष सितंबर के अंत तक इस योजना के लिए बजट के आवंटन 86,000 करोड़ का 60 प्रतिशत, केवल 51,600 करोड़ रुपए ही उपलब्ध होंगे. यह मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन को गंभीर तौर पर प्रभावित करेगा क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा, 21,000 करोड़ रपये पिछले वित्तीय वर्ष की लंबित देनदारियों के भुगतान में खर्च हुआ है. इस तरह के फैसले से ज़मीनी स्तर पर मांग के बावजूद मज़दूरों को मनरेगा में काम के लिए बेहिसाब तरीकों से हतोत्साहित किया जाएगा.
अपर्याप्त बजट- अधिकांश समस्याओं का मूल कारण
दरअसल मनरेगा को कमजोर करने में सबसे बड़ा कारण लगातार बजट में कमी और समय पर आबंटन राज्यों तक न पहुंचना ही है. इससे ही सभी तरह की समस्याएं पैदा होती है. फंड की कमी के चलते ही अघोषित तरीके से काम की मांग को नियंत्रित किया जाता है. अलग अलग तरीको से मज़दूरों को भी हतोत्साहित किया जाता है.
यह बात सरकार की संसदीय समिति की 2024 की एक रिपोर्ट में भी एक बड़ी कमजोरी के तौर पर चिन्हित की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘आवश्यकता के आधार पर संसाधनों की पूर्ति की जा सकती है’ लेकिन वर्ष के शुरुआत में अनुमानित बजट में ही फंड में कटौती करने से मनरेगा कार्यान्वयन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुयों पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. इसलिए कमेटी ने जमीनी स्तर पर इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए फंड की कमी एक बहुत बड़ी बाधा माना है. मनरेगा के लिए शुरू में ही उपयुक्त बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए जिसका आधार पिछले वर्ष के खर्च का चलन हो सकता है.
गौरतलब है कि पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी सहित देश के कई अर्थशास्त्रियों ने मनरेगा के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 2.64 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन सुझाया है. यहां तक कि अपनी एक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सिफारिश की है कि इस कार्यक्रम के लिए देश की जीडीपी का कम से कम 1.7% आवंटित किया जाना चाहिए.
इसके विपरीत, वर्ष 2024–25 में मनरेगा के लिए किया गया आवंटन जीडीपी का मात्र 0.26% ही है. इस वर्ष के बजट (2025–26) में भी केवल 86000 करोड़ रुपए ही मनरेगा के लिए रखे गए हैं. यह योजना की व्यापक जरूरतों और ग्रामीण भारत की बढ़ती आर्थिक असुरक्षा के संदर्भ में बेहद अपर्याप्त है. इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है. इसी तरह ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति ने 22 मई को संसद में प्रस्तुत अपनी आठवीं रिपोर्ट में यह उजागर किया कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में देरी अब भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है.
मजदूरी दरों की गणना में विसंगतियांं
संसदीय समिति ने मनरेगा के तहत मजदूरी को कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन करने की भी शिफारिश की है. समिति का मानना है कि वर्तमान दरें दैनिक बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त हैं और यह योजना ग्रामीण मज़दूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने उद्देश्य में विफल हो रही है. एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो काफी समय से यह समिति उठाती आ रही है वह है मनरेगा के अंतर्गत मज़दूरी दरों की गणना के विसंगतिपूर्ण तरीके के बारे में.
दरअसल मनरेगा के अंतर्गत मज़दूरी दरों की गणना खेत मज़दूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) के आधार पर की जाती है. अभी तक इसके लिए 1 अप्रैल 2009 की मूल दरों को आधार बनाकर संशोधन किया जाता है. संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस पद्धति की तीव्र आलोचना करते हुए कहा है कि ‘2009-2010 को आधार वर्ष मानकर की जा रही गणना अब अप्रासंगिक और निष्प्रभावी हो चुकी है, जो मौजूदा महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप कोई उचित आंकड़ा देने में असमर्थ है.’
इससे पहले यही तर्क महेंद्र देव समिति ने भी दिया था और सुझाव दिया गया था कि मनरेगा मज़दूरी सूचकांक का आधार वर्ष 2014 होना चाहिए. स्थायी समिति ने अपनी अनुशंसा में यह स्पष्ट रूप से कहा कि, ‘कम मज़दूरी दरों की समस्या का समाधान संभवतः आधार वर्ष और मूल दरों की समय के अनुरूप पुनर्समीक्षा तथा उनके यथोचित बढ़ोतरी के माध्यम से किया जा सकता है.’
अनूप सतपथी समिति ने भी सुझाव दिया था कि मनरेगा के अंतर्गत मज़दूरों को प्रतिदिन न्यूनतम 375 रुपये की मज़दूरी दी जानी चाहिए. लेकिन केंद्र सरकार ने संसद की अपनी ही स्थायी समिति की इस सिफारिश को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया, जिससे उसकी मंशा साफ़ झलकती है. इस वर्ष भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा की मज़दूरी की दरों में केवल 2% से 7% तक मामूली वृद्धि की है.
मनरेगा में कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने की जरुरत
संसदीय समिति ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 की जाए. यह लम्बे समय से चली आ रही एक मांग है लेकिन अभी तो 100 दिन के रोजगार की गारंटी होने के बावजूद प्रतिवर्ष काम के दिन औसतन 50 दिन प्रति परिवार से ऊपर नहीं जाते है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा के तहत भी प्रति परिवार औसतन कार्य दिवस केवल 50.18 ही है और कुल रजिस्टर्ड परिवारों में से केवल 7% परिवारों को ही वादा किए गए 100 दिनों का रोजगार मिल पाया है.
पश्चिम बंगाल में मनरेगा का संकट
पश्चिम बंगाल में मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत 2.56 करोड़ मज़दूर, जिनके पास जॉब कार्ड हैं और जो अकुशल मज़दूरी के लिए पूर्णतः पात्र भी हैं, पिछले तीन वर्षों से काम से महरूम हैं. इन मज़दूरों को ‘काम के कानूनी अधिकार’ से भ्रष्टाचार के आरोपों से कारण वंचित रखा जा रहा है. हालांकि यह सत्य है कि देश के अधिकांश राज्यों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, मनरेगा के क्रियान्वयन में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है. इसके पीछे ठेकेदारों, स्थानीय नेताओं, जिनमें अधिकांश सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से जुड़े हैं और विभिन्न स्तरों की नौकरशाही के बीच की सांठगांठ ज़िम्मेदार है.
भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में सबसे पहली आवश्यकता होती है मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, जो न तो केंद्र सरकार में दिखाई देती है और न ही पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में. केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से हल करने के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए भ्रष्टाचार के नाम पर टीएमसी सरकार को निशाना बना रही है. वहीं टीएमसी सरकार खुद को पीड़ित बताकर ग्रामीण गरीबों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है. परिणामस्वरूप, सबसे अधिक पीड़ित वे मेहनतकश मज़दूर हो रहे हैं जो न तो भ्रष्टाचार के ज़िम्मेदार हैं और न ही इसके पक्षधर, लेकिन उन्हें अपने ही कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया गया है.
अब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 1 अगस्त 2025 से पश्चिम बंगाल में मनरेगा का काम शुरू करने के निर्देश दिए है.
गुजरात में मनरेगा घोटाले, भाजपा के दोहरे मापदंड
पिछले कुछ दिनों में भाजपा की भ्रष्टाचार की लड़ाई के मॉडल की पोल देश की जनता के सामने खुल गई है. लड़ाई तो दूर की बात है लेकिन भाजपा के नेता भ्रष्टाचार के नित नए कीर्तिमान बना रहे है. पिछले कुछ महीनो में पूरे देश में भाजपा के विकास मॉडल के रूप में प्रचारित राज्य गुजरात में मनरेगा में हो रहे कई सौ करोड़ रुपये के घोटाले उजागर हुए है.
ऐसे ही एक मामले में गुजरात के दाहोद ज़िले में राज्य के पंचायत और कृषि मंत्री बचू खाबड़ के बेटे बलवंत खाबड़ को दाहोद पुलिस ने मनरेगा में 70 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ़्तार किया है.
प्रारंभिक खुलासों में यह सामने आया है कि यह घोटाला पूरी तरह एक फर्जी नेटवर्क पर आधारित था, जिसमें सड़कों, बांधों और अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों जैसे अधोसंरचना परियोजनाओं को केवल कागज़ों पर दिखाया गया था. मनरेगा के अंतर्गत आदिवासी समुदायों के लिए नियोजित रोजगार से जुड़ी धनराशि को कथित रूप से जाली दस्तावेज़ों के माध्यम से चुराया गया और इसे उन एजेंसियों को भेजा गया जिनका संबंध मंत्री के बेटों से था. इस घोटाले में मंत्री बचू खाबड़ के दोनों बेटे, बलवंत और किरण शामिल पाए गए हैं.
पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकारों की वास्तविक मंशा को समझने के लिए यह जरूरी है कि सोशल ऑडिट की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाए. हालांकि, जो सरकारें और राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा करते हैं, वे अक्सर खुद सोशल ऑडिट से बचते नजर आते हैं. मनरेगा जैसी योजनाओं में पारदर्शिता लाने वाला यह तंत्र उनके लिए असहज होता है.
सोशल ऑडिट टीम के सदस्यों को डराना-धमकाना, उनके खिलाफ हिंसा और झूठी रिपोर्ट तैयार करने का दबाव डालना आम बात हो गई है. पिछले दशक में भाजपा सरकार का मनरेगा को लागू करने का रिकॉर्ड बेहद निराशाजनक रहा है. यह स्पष्ट रूप से मनरेगा की मूल भावना सरकार के निरंतर हमलों को दर्शाता है. मनरेगा को लगातार कमजोर करना भारत के मेहनतकश लोगों द्वारा अर्जित रोजगार के अधिकार पर एक संगठित हमला है.
(लेखक अखिल भारतीय कृषि मजदूर संघ के संयुक्त सचिव हैं.)