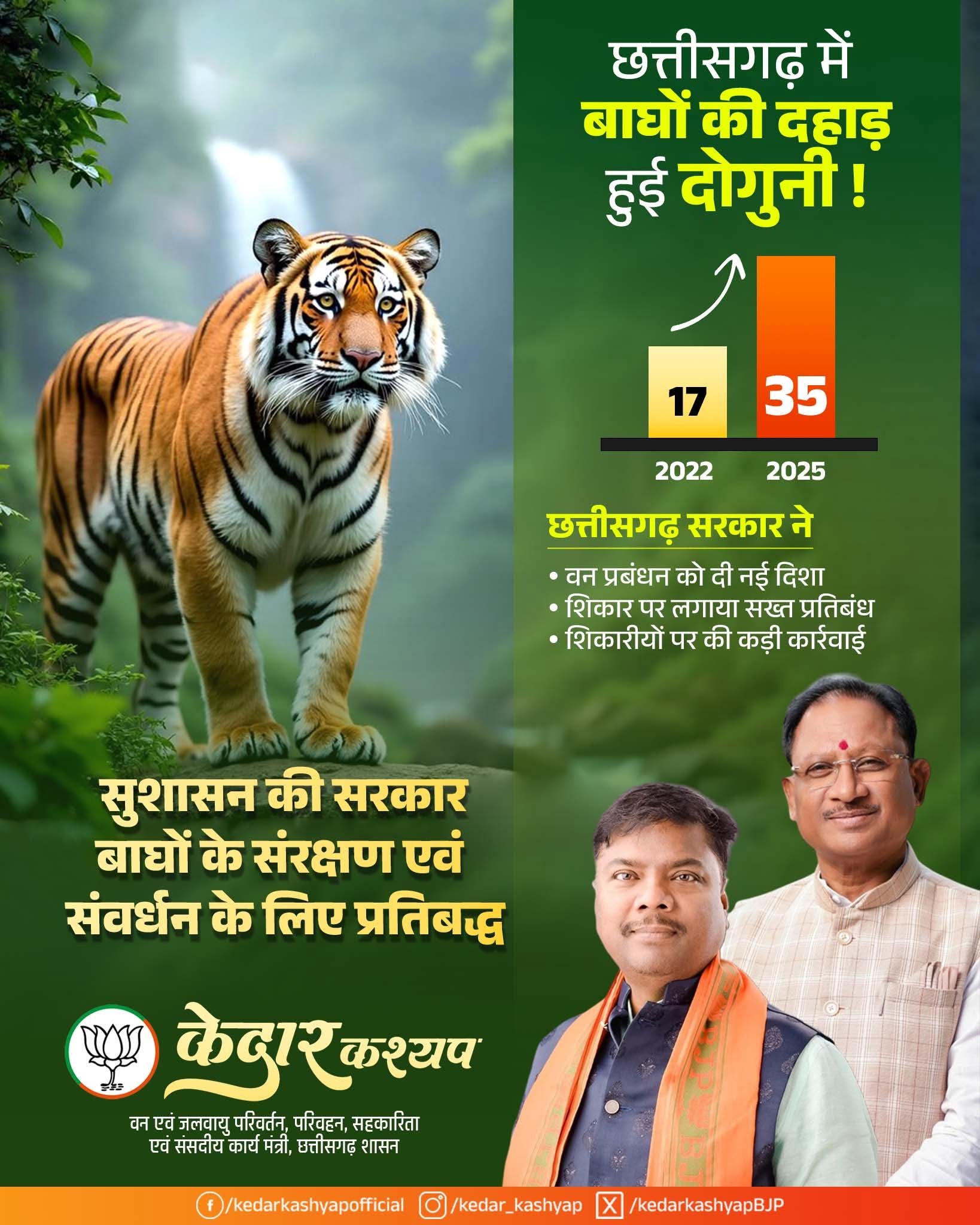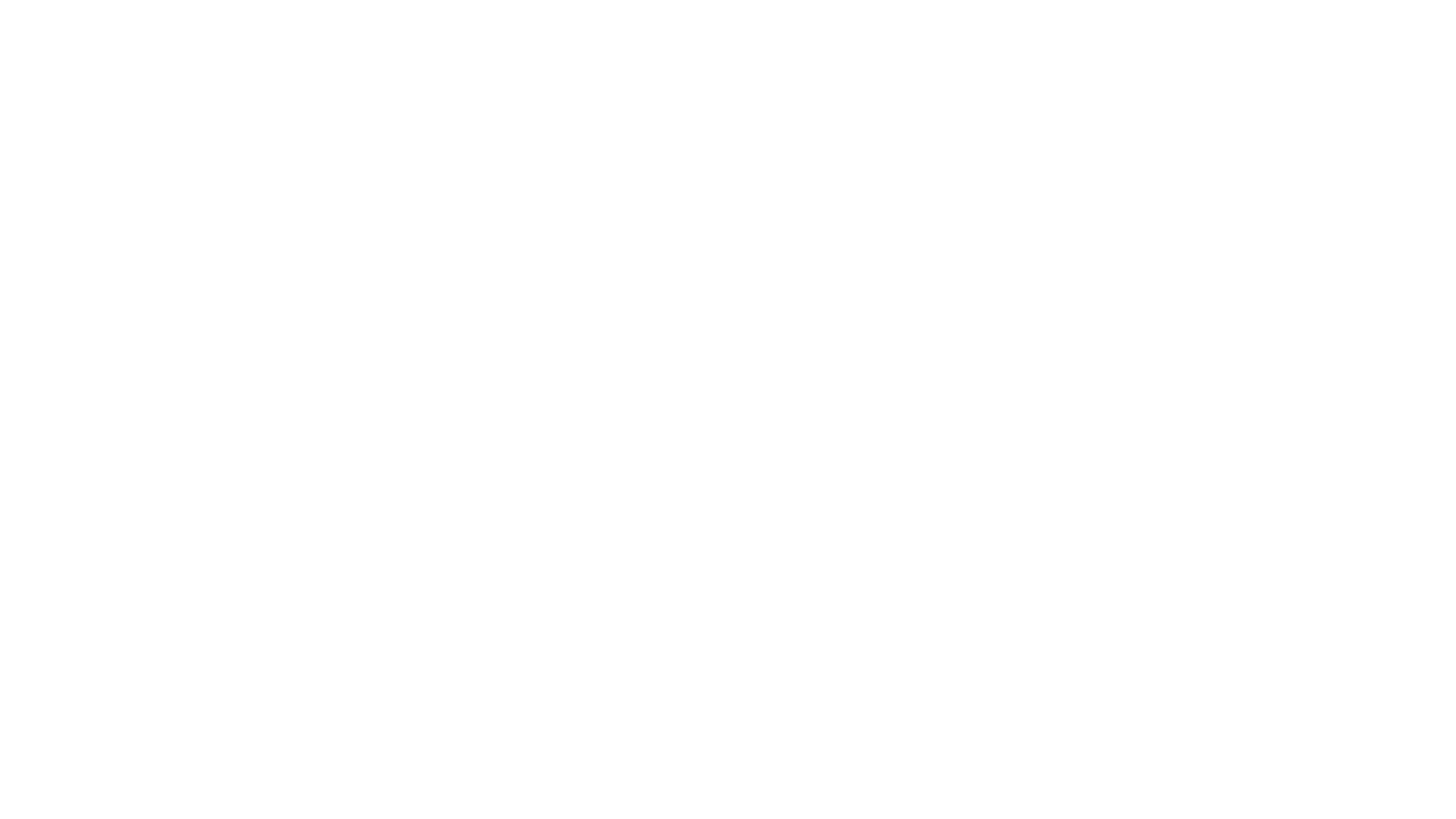(भारतीय मुस्लिमों पर दो लेखों की श्रृंखला की यह पहली क़िस्त है.)
भारत में 200 मिलियन मुसलमान रहते हैं. इंडोनेशिया और पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में यहां ज़्यादा मुसलमान रहते हैं. फिर भी, 2023 में, स्वतंत्र भारत में 1952 में हुए पहले आम चुनाव के बाद पहली बार, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) – संसद में पूर्ण बहुमत होने और देश के 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से 15 में अकेले या गठबंधन में शासन करने के बावजूद – मुस्लिम प्रतिनिधित्व का लगभग पूर्ण अभाव था.
पार्टी के पास संसद के किसी भी सदन या लगभग सभी राज्य विधानसभाओं में कोई निर्वाचित मुस्लिम सदस्य नहीं था. एकमात्र अपवाद थे ग़ुलाम अली, जो राज्यसभा के एक मनोनीत सदस्य थे, और तफ़ज्जल हुसैन, त्रिपुरा विधानसभा में भाजपा के एकमात्र मुस्लिम विधायक – सभी राज्यों में पार्टी के 1,658 विधायकों में से सिर्फ़ एक. और, भारत के आज़ाद होने के बाद पहली बार, राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं था.
देश के निर्वाचित नेतृत्व ने इस बहिष्कार के साथ दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के 200 मिलियन मुसलमान नागरिकों को सख़्त और स्पष्ट संदेश दिया है: राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए हमें आपके वोटों की आवश्यकता नहीं है.
भाजपा के वैचारिक अभिभावक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के विचारकों ने लगभग सौ साल पहले अपने गठन के समय से ही बहुलतावादी भारत को एक हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित करने का समर्थन किया है ,जिसमें मुसलमानों (और ईसाइयों) को केवल दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में रहने की ‘अनुमति‘ दी जाएगी. भाजपा के नियंत्रण वाले किसी भी निर्वाचित कार्यालय से मुसलमानों की पूर्ण अनुपस्थिति से उनकी नागरिकता में गिरावट का संकेत मिलता है, जिस नागरिकता का महत्व पहले ही कम हो गया है.
आरएसएस और भाजपा की हिंदू बहुसंख्यक राजनीति की जीत ने भारत के मुसलमानों को -जो संवैधानिक रूप से इस देश के समान नागरिक हैं – देश की शासन व्यवस्था में भागीदारी से बाहर करने के उनके लक्ष्य के सबसे अधिक क़रीब पहुंचा दिया. इस परिघटना से भारतीय गणतंत्र की यात्रा में एक दुखद पड़ाव को रेखांकित किया जा सकता है. भारतीय मुसलमानों को चुनावी रूप से नकार दिए जाने के बाद उन्हें राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक बना दिया गया है; कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़कर उन्हें राजनीतिक बोझ मानने लगे हैं.
भारत के मुसलमानों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया जाना कोई आकस्मिक घटना नहीं है, हालांकि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इसकी गति बहुत तेज़ हो गई है.
भारत के विभाजन के समय इसके पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर दो बड़े भूभाग अलग हो गए थे
1947 में भारत के विभाजन के समय इसके पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर दो बड़े भूभाग अलग हो गए थे, जहां मुसलमानों की संख्या अधिक थी. जिन मुसलमानों ने भारत में रहने का विकल्प चुना उनकी आबादी तो अधिक थी मगर वे भौगोलिक रूप से बिखरे हुए थे. देश के संविधान का मसौदा तैयार करते समय भारत की संविधान सभा ने तीन कमज़ोर और वंचित समुदायों: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुसलमानों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के तरीक़ों पर विस्तार से चर्चा की.
अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विचार पूरी तरह से ख़ारिज कर दिया गया, लेकिन संविधान सभा ने विशेष समुदायों के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण पर विचार किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वंचित समूहों को उनकी आबादी के अनुपात में संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व मिले.
संविधान के शुरुआती मसौदों में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों, सरकारी नौकरियों और यहां तक कि मंत्रिमंडल में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के प्रावधान थे, लेकिन अंतिम मसौदे में मुसलमानों को सभी राजनीतिक सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को मंज़ूरी दी गई, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं.
राजनीतिक विश्लेषक शेफ़ाली झा ने इस बात पर विचार किया है कि कैसे संविधान सभा के सदस्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की तुलना में उन्हें विशेष राजनीतिक अधिकार दिए जाने के स्पष्ट विरोधी थे. कुछ सदस्यों को डर था कि विभाजन के बाद की परिस्थितियों में सरकारी नौकरियों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण संभावित रूप से विभाजनकारी होगा.

भारत में बहुमत एक राजनीतिक नहीं बल्कि सांप्रदायिक इकाई है
बीआर आंबेडकर, जिन्होंने संविधान का ड्राफ़्ट तैयार करने वाली कमिटी का नेतृत्व किया, अपनी अंतर्दृष्टि में उल्लेखनीय रूप से दूरदर्शी थे कि भारत में बहुमत एक राजनीतिक नहीं बल्कि सांप्रदायिक इकाई है. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में, बहुमत मुद्दों और नीतियों द्वारा ‘तैयार होता’ है; भारत में, बहुमत – यानी हिंदू बहुमत – ‘पैदाइशी‘ है, और इसलिए सांप्रदायिक है, जो स्वाभाविक रूप से अन्य जाति, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है.
आंबेडकर की अंतर्दृष्टि इस तथ्य से और अधिक स्पष्ट हो जाती है कि संविधान के अंतिम प्रारूप में जातिगत और जनजातीय अल्पसंख्यकों के लिए राजनीतिक सुरक्षा शामिल की गई, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यकों को इससे बाहर कर दिया गया.
लोकसभा में बिना किसी आरक्षण के निष्पक्ष मुस्लिम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती थी – भारतीय संसद का निचला सदन, जिसके सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर फ़र्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली के तहत चुने जाते हैं. ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वतंत्रता के समय भी भारतीय आबादी का लगभग 10 प्रतिशत होने के बावजूद मुसलमानों के पास बहुत कम निर्वाचन क्षेत्र थे जहां वे अकेले चुनावी नतीजे तय कर सकते थे – भले ही किसी क्षेत्र के सभी मुस्लिम एक ही उम्मीदवार को वोट देते हों.
आज 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से केवल 15 में ही मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है. यह एक गंभीर वास्तविकता है कि भारत के 97 प्रतिशत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं. इसके अलावा, केवल दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर, तथा लक्षद्वीप – में ही उनका बहुमत है और देश के किसी भी राज्य में नहीं हैं. (जम्मू और कश्मीर, जो पहले भारत का एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य था, जिसे 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और नई दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के सीधे शासन के अधीन कर दिया गया).
उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उनकी संख्या काफ़ी अधिक है, हालांकि अभी भी बहुमत से बहुत कम है, और असम, केरल तथा तेलंगाना में कम महत्वपूर्ण लेकिन अभी भी पर्याप्त आबादी है. जैसा कि राजनीतिक वैज्ञानिक अदनान फ़ारूक़ी ने समझाया कि इसका मतलब यह है कि भारत में मुसलमान बिखरे हुए अल्पसंख्यक हैं, बल्कि यह भी कि वे अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में बहुत अधिक संख्या में हैं.
इसलिए, स्वतंत्रता के समय की तरह आज भी भले ही मुसलमानों ने एक समूह के रूप में मतदान किया हो – और बहुत से शोध से इस बात की पुष्टि होती है कि वे ऐसा नहीं करते हैं – वे केवल मुट्ठी भर निर्वाचन क्षेत्रों में ही चुनावी नतीजों को ख़ुद से प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि, यह अपने आप में नए स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत में मुसलमानों की महत्वपूर्ण राजनीतिक भागीदारी की संभावना को ख़त्म नहीं करता. इसका मतलब यह है कि मुस्लिम मतदाताओं को ग़ैर-मुस्लिम पार्टियों, और ग़ैर-मुस्लिम मतदाताओं के साथ भी सार्थक और प्रभावी गठबंधन बनाने की आवश्यकता होगी जो वैचारिक रूप से उनके प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया न रखते हों.
मुस्लिम-पहचान वाली राष्ट्रीय पार्टियों का कोई भविष्य नहीं है
इसका पहला निहितार्थ यह था कि मुस्लिम-पहचान वाली राष्ट्रीय पार्टियों का कोई भविष्य नहीं है – जो मुसलमानों से मुसलमान के रूप में मतदान करने का आह्वान करतीं, जो भारतीय मुसलमानों के बीच के भाषाई, संस्कृतिक, लैंगिक, जातिगत और वर्गीय विविधता को पृष्ठभूमि में डालकर धार्मिक पहचान के साझा हितों को आगे करने की वकालत करतीं. परिणामस्वरूप, आज भारत में मुस्लिम लीग जैसी कोई राष्ट्रीय मुस्लिम पार्टी नहीं है, जो विभाजन से पहले एक प्रमुख राजनीतिक ताक़त थी.
मौजूदा समय में कुछ मुस्लिम बहुल पार्टियों का प्रभाव सिर्फ़ कुछ भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित है: केरल में दो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ़्रंट और तेलंगाना में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन. जब ये अपने स्थानीय प्रभाव क्षेत्र के बाहर उम्मीदवार उतारते हैं तो इन्हें बहुत मामूली चुनावी समर्थन मिलता है.
दूसरा निहितार्थ यह है कि मुसलमानों से अक्सर अन्य समुदायों के मतदाताओं के साथ मिलकर ग़ैर-मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट देने के लिए कहा जाएगा, उनके इस आकलन के आधार पर कि कौन सा राजनीतिक दल और उम्मीदवार उनके हितों की सबसे अच्छी तरह से रक्षा कर सकता है और उनके लिए सहायक हो सकता है.
यह एम एस सथ्यू की एक प्रतिष्ठित फ़िल्म गर्म हवा की याद दिलाता है. जिसमें आगरा के एक वयोवृद्ध मुसलमान की मार्मिक व्यथा को दर्शाया गया है, जो पाकिस्तान नहीं जाने का दृढ़ निश्चय करता है, मगर निरंतर संदेह और भेदभाव उसे अंततः पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर कर देता है.
फ़िल्म के अंतिम दृश्य में, जब नायक पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए तांगे पर सवार होकर रेलवे स्टेशन जा रहा होता है, तो वह प्रदर्शनकारियों के एक जुलूस को देखता है, जो लाल झंडा लहरा रहा है, हरा झंडा नहीं, इसे रेखांकित किया जाना चाहिए. वह तांगे से उतरता है और ड्राइवर से अपने वापस घर लौटने के लिए कहता है, जबकि वह ख़ुद जुलूस में शामिल हो जाता है.

भारतीय मुसलमान की भारत में पहचान
इस तरह, फ़िल्म यह पुष्टि करती है कि भारतीय मुसलमान का भारत में एक राजनीतिक भविष्य है, जो इस्लाम के अनुयायी की पृथक पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पहचान एक भारतीय नागरिक की भी है जो न्याय और समानता के लिए सामूहिक संघर्ष में अन्य भारतीयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है.
यह रेखांकित करना भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय मुसलमानों और अन्य पहचान वाले भारतीयों ने स्वतंत्रता के बाद के दशकों में यह सीखा कि जिस व्यक्ति को वे चुनते हैं, वह किसी भी विशेष धर्म, जाति या लिंग की पहचान का हो सकता है, लेकिन एक बार चुने जाने के बाद वह न केवल अपनी पहचान के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में हर पहचान के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है.
इन तरीक़ों से भारतीय मुसलमानों ने चुनावी राजनीति में प्रभावी और ऊर्जावान ढंग से भाग लेना सीखा, भले ही उन्हें ऐतिहासिक रूप से वंचित अन्य समुदायों की तरह आरक्षण का लाभ न मिला हो, और पर्याप्त संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी संगठित आबादी न हो, जो चुनाव परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सके.
इन आधारों पर भारत के राजनीतिक दलों ने – आरएसएस से संबद्ध भारतीय जनसंघ, जो बाद में भाजपा बना, इसका एक अपवाद है – स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में चुनावी लोकतंत्र में मुस्लिम नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया, हालांकि आधे-अधूरे तरीक़े से; और इस तरह मुस्लिम नागरिकों ने भारतीय लोगों के महान लोकतांत्रिक एडवेंचर में भाग लिया.
हालांकि, यह बदल गया है. संसद और राज्य विधानसभाओं में चुने गए मुसलमानों की बढ़ती संख्या अपनी कहानी ख़ुद बयां करती है.
फ़ारूक़ी ने विस्तार से बताया है कि 1952 में भारत के पहले आम चुनाव से लेकर 2019 के आम चुनाव तक, औसतन, लगभग 5 प्रतिशत मुसलमान उम्मीदवार लोक सभा के लिए चुने गए. स्वतंत्रता के समय मुसलमानों की संख्या भारतीय आबादी का 9 प्रतिशत से अधिक थी, और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 14 प्रतिशत थी – जो आज तक की अंतिम जनगणना है. इसलिए, लोकसभा में मुसलमानों की आनुपातिक उपस्थिति ऐतिहासिक रूप से, मोटे तौर पर, मुस्लिम आबादी के आधे से एक तिहाई के बीच रही है.
भारत के राजनीतिक इतिहास में चार चरण
फ़ारूक़ी लोकतांत्रिक भारत के राजनीतिक इतिहास में चार चरणों की पहचान करते हैं. पहला चरण 1952 में होने वाले पहले आम चुनाव से 1971 तक चला, और इस पहले चरण में एक ही प्रमुख राजनीतिक दल का वर्चस्व रहा: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस. दूसरा चरण, 1977 से 1989 तक का है, जिस चरण में कांग्रेस का पतन हुआ और वह फिर से उभरी.
1989 से 2014 तक के तीसरे चरण को मुख्य रूप से तीन बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है: कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष चुनावी समर्थन में गिरावट, अपने अधिक सांप्रदायिक समर्थन वाले अधार वोट के साथ भाजपा के लगातार उभार और कांग्रेस के पतन से ख़ाली हुई जगह को वंचित-जाति या क्षेत्रीय जनाधार वाली कई छोटी पार्टियों द्वारा भरा जाना. और चौथा चरण, 2014 के बाद से, चुनावी राजनीति में एक राजनीतिक दल का वर्चस्व फिर से स्थापित होता है: इस बार, दक्षिणपंथी, हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा.
यह देखना दिलचस्प है कि प्रत्येक चरण में संसद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व किस तरह विकसित हुआ. फ़ारूक़ी का आकलन है कि पहले चरण में मुस्लिम पहचान वाले लोकसभा प्रतिनिधियों की संख्या सदन में औसतन 5 प्रतिशत थी – जो मुस्लिम आबादी के अनुपात में लगभग आधी थी क्योंकि तब देश में मुसलमान आबादी की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत थी.
1977 से 1989 के दूसरे चरण में उनकी उपस्थिति चरम पर थी, जिस दौरान कांग्रेस पहली बार हारी और फिर 1984 में अपने सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रदर्शन तक पहुंची. इस दौरान सदन में 8 प्रतिशत सांसद मुसलमान थे, जो उनकी जनसंख्या में हिस्सेदारी के अनुपात के क़रीब थी, जो 11 प्रतिशत पर बनी रही.
तीसरे चरण में, जो क्षेत्रीय दलों के गठबंधन और भाजपा के लगातार उदय का दौर था, 1989 से 2014 तक, लोकसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 6 प्रतिशत तक गिर गया, और 2019 में, जब मोदी की भाजपा ने फिर से चुनाव में जीत हासिल की, तो इसमें मामूली सुधार ही हुआ. अब सदन में मुसलमान सांसदों की संख्या क़रीब 4 फ़ीसदी है, जबकि आबादी में उनकी हिस्सेदारी क़रीब 14 फ़ीसदी है.
संसद में मुसलमान सांसदों की भागीदारी
जैसा कि समाज विज्ञानी इक़बाल ए. अंसारी बताते हैं, पहले चरण के दैरान जब निर्विवाद रूप से कांग्रेस का प्रभुत्व था तब कुल मुसलमान लोक सभा सांसदों में से 71 फ़ीसदी सांसद कांग्रेस के थे; फिर अगले दो चरणों में यह भागीदारी घटकर क्रमश: 58 फ़ीसदी और 33 फ़ीसदी रह गई. इन बाद के चरणों में, उभरते क्षेत्रीय दलों के मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या ने कांग्रेस के मुस्लिम प्रतिनिधित्व की संख्या में आई गिरावट की भरपाई की.
लेकिन 2014 में, जब कांग्रेस लोकसभा में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई, और सदन में उसकी कुल हिस्सेदारी सिर्फ़ 8 फ़ीसदी रह गई, तो उसी अवधि में क्षेत्रीय दलों के मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई. यहां तक कि उत्तर प्रदेश में, जहां किसी भी भारतीय राज्य की तुलना में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, वहां से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया.
संयोग से, 15 प्रतिशत से अधिक मुसलमान आबादी वाले भारतीय राज्यों – केरल, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा (राज्य का दर्जा छीने जाने से पहले) जम्मू और कश्मीर – ने आम तौर पर लोकसभा में बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रतिनिधि भेजे हैं.

मुसलमानों के उच्च अनुपात वाले अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश और झारखंड नकारात्मक अपवाद के रूप में उभरे हैं. उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों में मुसलमानों का अनुपात 1980 के दशक की शुरुआत में 18 प्रतिशत था, लेकिन 2014 में इस राज्य से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चुना गया. सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद से चार कार्यकालों, यानी 2004, 2009, 2014 और 2019 में केवल एक मुस्लिम सांसद लोकसभा पहुंचा है.
और फिर उच्च मुस्लिम आबादी वाले कई राज्य हैं जिन्होंने शुरू से ही मुस्लिम प्रतिनिधियों के मामले में एक तरह की राजनीतिक अस्पृश्यता बनाए रखी है. उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 14 प्रतिशत है, त्रिपुरा में 9 प्रतिशत, तथा मणिपुर और गोवा में 8 प्रतिशत – फिर भी इन सभी राज्यों से कभी कोई मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं चुना गया.
गुजरात, जिसकी 9 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है, वहां की राज्य विधानसभा में सिर्फ़ एक मुस्लिम विधायक है, तथा 1984 के बाद से लोकसभा के लिए एक भी मुस्लिम को नहीं चुना गया है.
हालांकि, फ़ारूक़ी और राजनीतिक वैज्ञानिक ई श्रीधरन ने यह भी बताया है कि कैसे 2018 तक ग़ैर-भाजपाई राजनीतिक दलों ने राज्यसभा– भारतीय संसद का ऊपरी सदन, जिसकी सदस्यता काफ़ी हद तक राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से निर्धारित होती है – में अपनी उपस्थिति का इस्तेमाल लोकसभा में मुसलमानों के कम प्रतिनिधित्व की भरपाई के लिए किया.
मुसलमानों की अधिक उपस्थिति का तीन तरीक़ों से मूल्यांकन
विद्वान हिलाल अहमद राज्यसभा में तुलनात्मक रूप से मुसलमानों की अधिक उपस्थिति का तीन तरीक़ों से मूल्यांकन करते हैं: (क) इससे धर्म-आधारित आरक्षण की धारणा को ज़ाहिर किए बिना, एक सामाजिक श्रेणी के रूप में मुसलमान का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व होता है; (ख) इससे लोकतंत्र की मज़बूती सुनिश्चित होती और (ग) इससे उन विचारों और दावों की पुष्टि में मदद मिलती है जो चुनावी मुद्दे नहीं बन पाते हैं.‘
1952 से 1977 तक, कुल 1381 निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों में से 137 मुसलमान थे. इसका मतलब यह हुआ कि सदन में मुसलमानों की संख्या लगभग 10 प्रतिशत थी – यह आंकड़ा आबादी में उनकी 11 प्रतिशत हिस्सेदारी से थोड़ा कम है. 1977 से 1989 तक, कुल 451 निर्वाचित सदस्यों में से 40 मुसलमान थे; इस अवधि में भी सदन में 10 प्रतिशत मुसलमान सांसद चुने गए, जबकि इस अवधि में उनकी आबादी 12 प्रतिशत थी.
1990 से 2018 के बीच भी कमोबेश यही स्थिति रही या उससे बेहतर ही हुई, इस अवधि में राज्यसभा में मुसलमान प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी उनकी आबादी के अनुपात से मेल खाती है, जो 13 प्रतिशत है. इस अवधि में, 869 निर्वाचित सदस्यों में से 112 मुसलमान थे.
फिर भी यह उल्लेखनीय है कि कांग्रेस, जो पहले अधिकतर मुस्लिम सांसद को चुनकर राज्यसभा भेजती थी, इस अंतिम चरण में उनकी संख्या पहले की तुलना में बहुत कम थी: कांग्रेस से 10, सपा से 3, भाजपा, जेकेपीडीपी और एआईटीसी से 2-2, तथा जेडी(यू), आईयूएमएल, बीएसपी और एनसीपी से एक-एक विधायक शामिल हैं.
जब इन दो मुस्लिम भाजपा प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो पार्टी ने उनकी जगह ग़ैर-मुस्लिमों को लाने का फ़ैसला किया, और दोनों सदनों में अपने संसदीय दल से इस प्रतीकात्मक मुस्लिम प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया.
राज्य विधानसभाओं में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है. उत्तर प्रदेश विधानसभा में, मुस्लिम आबादी के मामले में सबसे बेहतर प्रतिनिधित्व 2012 में मिला था: लगभग 19 प्रतिशत की आबादी वाले मुसलमानों के हिस्से में विधान सभा की 17 प्रतिशत सीटें आई थीं.
अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो 1977, 1985 और 2007 में यह प्रतिनिधित्व 11 से 14 प्रतिशत के बीच देखा गया, जिसे उच्च स्तर कहा जा सकता है, जबकि 1967, 1991 और 2017 में यह प्रतिनिधित्व गिरकर 6 प्रतिशत या उससे कम पर आ गया, इसे निम्न स्तर कहा जाएगा. राज्य के 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व 8.7 प्रतिशत तक पहुंच गया, लेकिन 19.5 प्रतिशत की मुस्लिम आबादी के मुक़ाबले में इसे कम ही कहा जाएगा.
एक और उदाहरण असम है, जहां किसी भी भारतीय राज्य के मुक़ाबले मुसलमानों का अनुपात सबसे अधिक है. (एक राज्य के रूप में पहले सबसे अधिक अनुपात जम्मू-कश्मीर में था, मगर अब इससे राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है.)
असम विधानसभा में 1983 में मुसलमानों का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व देखने को मिला, जब यह आंकड़ा मुसलमानों की स्थानीय आबादी से मेल खाता था जो कि 26 प्रतिशत था. सबसे कम प्रतिनिधित्व 1962 में देखने को मिला, जब प्रतिनिधित्व 12.4 प्रतिशत था और आबादी का अनुपात लगभग इससे दोगुना.
मौजूदा राज्य विधानसभा में 24.6 प्रतिशत मुसलमान हैं, जबकि आबादी में उनकी हिस्सेदारी 38 प्रतिशत है. चौंकाने वाली बात यह है कि मौजूदा मुस्लिम प्रतिनिधियों में से एक भी भाजपा से नहीं है, जो सदन में अब तक की सबसे बड़ी पार्टी है.
सभी मुस्लिम विधायक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ़्रंट (एआईयूडीएफ़) से हैं – एआईयूडीएफ़ को व्यापक रूप से बंगाली मूल के असमिया मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाला दल माना जाता है.
(इस लेख को लिखने के लिए ओमैर ख़ान और बदरे आलम द्वारा किए गए शोध से सहायता मिली है.)
(मूल अंग्रेज़ी से ज़फ़र इक़बाल द्वारा अनूदित. ज़फ़र भागलपुर में हैंडलूम बुनकरों की‘कोलिका’नामक संस्था से जुड़े हैं.)