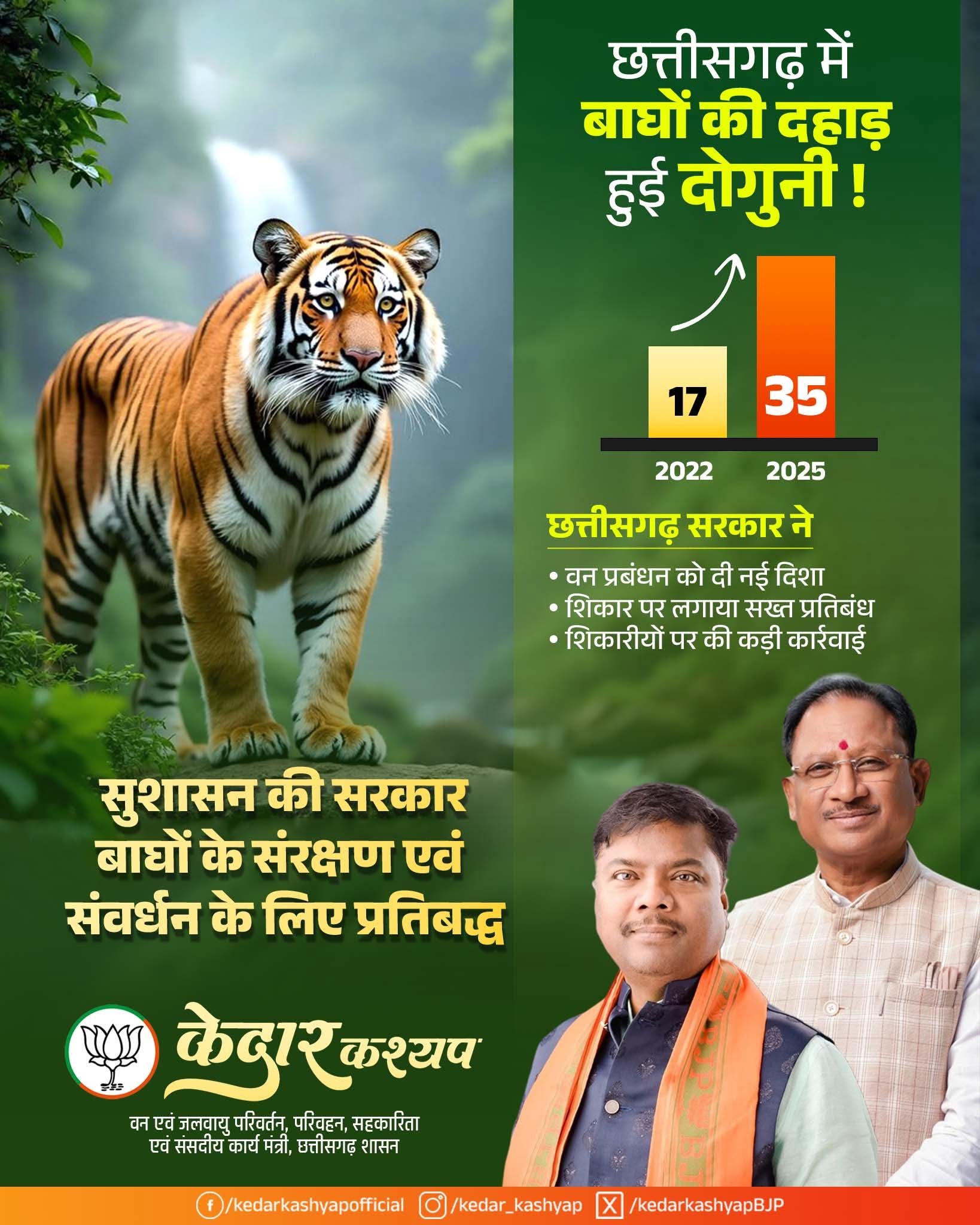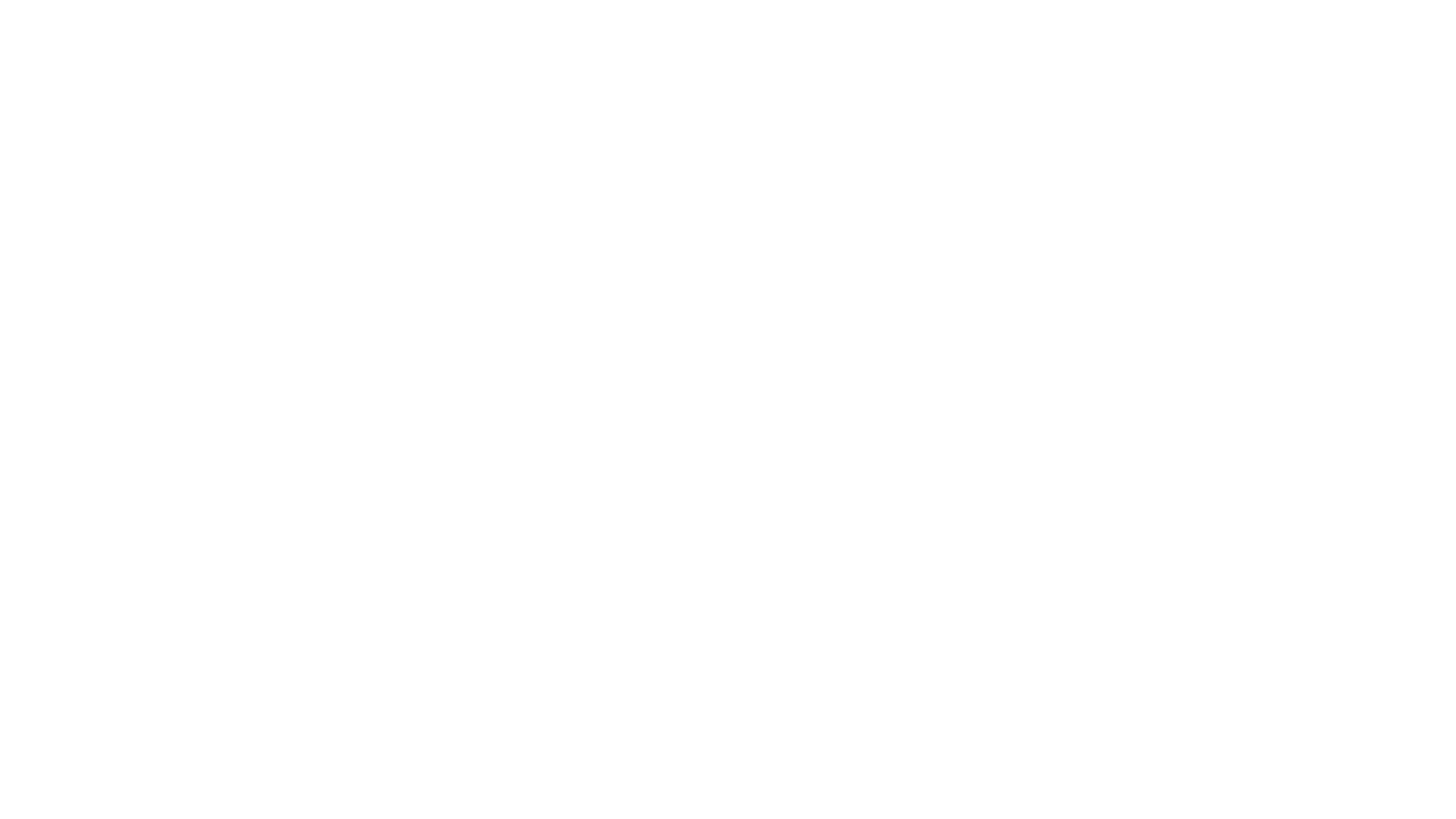आस्था और हिंसा में संबंध काफ़ी प्राचीन है. ऐसा भी रहा है कि धर्म के नाम पर की गई हिंसा को हिंसा नहीं माना जाता रहा. प्रसिद्ध उक्ति थी: ‘वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति’ धर्मचिंतन में हिंसा का विरोध भी होता रहा है. भक्ति काल में धर्म और अध्यात्म का जो व्यापक जनजांत्रिकीकरण हुआ उसने, अलबत्ता, काफ़ी हद तक, समरसता-सद्भाव-संवाद-समझ का परिवेश बनाया-पोसा. उसे औपनिवेशिक सत्ता ने अपनी शक्ति की प्रतिष्ठा और विस्तार के लिए खण्डित और बाधित किया.
उसका प्रतिकार महात्मा गांधी ने एक अहिंसक स्वतंत्रता-आंदेलन का नेतृत्व कर लिया. पर वे स्वयं स्वतंत्र भारत में एक हिंदू हत्यारे की गोलियों का शिकार हुए. देश की स्वतंत्रता बंटवारे की क़ीमत पर मिली और बंटवारे के समय व्यापक हिंसा हुई. भारतीय लोकतंत्र में हिंसा थमी नहीं और वह कई नए क्षेत्रों जैसे भाषा, मीडिया, फ़ैशन, सिनेमा, सामाजिक व्यवहार आदि में फैलती गई है.
इन दिनों शिवभक्तों की कांवड़ यात्राएं चल रही हैं जिनमें ये भक्त अपनी धार्मिक आस्था को लगातार हिंसक और उपद्रवी बना रहे हैं. रास्ते में पड़नेवाली दूकानों की लूटपाट, वाहनों की तोड़-फोड़, मार-पीट, गालीगलौज आदि की घटनाएं रोज़ घट रही हैं. इन भक्तों की आस्था के बारे में शंका करना शायद उपयुक्त न होगा. जैसी भी वह है, उसका उन्हें अधिकार है. पर यह चिंताजनक है कि आस्था के नाम पर ऐसी हिंसा की रोकथाम करने के बजाय हिंदुत्व की जमातें और राजसत्ताएं उन पर पुष्पवर्षा करती हैं.
हर वर्ष कांवड़ यात्राएं होती हैं: उनके लिए सार्वजनिक धन से विश्राम शिविर बनाए जाते हैं; चिकित्सा, सुचारु यातायात आदि की व्यवस्था होती है. हर वर्ष हिंसा की घटनाएं भी होती हैं. उनमें कमी आने के बजाय बढ़ोतरी होती रहती है. इस हिंसक दबंगई के अनुष्ठान को हिंदू धर्म के किसी चिंतन या प्रवृत्ति से कैसे उचित ठहराया जा सकता है, यह समझ से बाहर है.
इन कांवड़ियों में कुछ सच्चे भक्त भी होंगे ज़रूर. पर उनमें नेतृत्व लफंगों के हाथ चला गया है, जो शिवभक्त कम, हिंदुत्व नामक राजनैतिक विचारधारा के ध्वजाधारी अधिक हैं. सारे रास्ते आम नागरिकों के लिए यह यात्रा कितनी विरूप, आक्रामक और असह्य होती जाती है यह स्पष्ट है. यह एक स्तर पर धर्मद्रोह के बराबर है.
लूटपाट, उपद्रव और उद्दण्डता, मुफ़्तख़ोरी, झगड़े-झांसे, नफ़रत और हिंसा किस हिंदू धर्म का हिस्सा या अभिव्यक्ति हैं? यह हिंदू धर्म की नई विडंबना है कि उसके नाम पर, उसके भक्त-अनुयायी, राजनैतिक उन्माद में हिंदू धर्म को विकृत, विरूपित और खण्डित कर रहे हैं.
‘तुका आकाश जितना’
यों तो भक्ति काव्य एक अखिल भारतीय परिघटना था, लेकिन उसके सभी कवियों की अखिल भारतीय कीर्ति नहीं हो पाई, मुख्यतः भाषाओं की बहुलता के कारण. मराठी के संतकवि तुका राम को संयोग से, ऐसी कीर्ति मिल पाई. उनके पहले भी हिंदी में अनुवाद हुए हैं. उनकी मराठी समाज में उपस्थिति उतनी ही व्यापक और निरन्तर है जितनी कबीर और तुलसी की हिंदी में.
कवि और हिंदी के संभवत: सबसे सर्जनात्मक कार्टूनिस्ट राजेंद्र धोड़पकर ने उनके कुछ अभंगों का नया हिंदी अनुवाद किया है और वह पुस्तकाकार ‘तुका आकाश जितना’ नाम से रूख़ पब्लिकेशन्स ने प्रकाशित किया है.
तुकाराम के यहां प्रायः संक्षेप पर आग्रह और उसका अद्भुत काव्यकौशल है. एक तरह का चुटीलापन जो सुनने-पढ़नेवाले पर बोझ नहीं डालता. जिस कविता के शीर्षक से पुस्तक का नाम दिया गया है वह छोटी और मर्मस्पर्शी है:
अणु-परमाणु से भी छोटा तुका
हो गया आकाश जितना.
छोड़ दी त्रिपुटी
दीप जल उठा घटी.
निगलकर छोड़ दिया कलेवर
जो था अब भ्रम का आकार.
तुका कहे, अब बस
बचा हूं परोपकार भर.
भक्त कवि के यहां, प्रायः सभी के यहां, कॉस्मिक चेतना और बिम्ब हैं. ‘आकाश मण्डप पृथ्वी आसन’ कविता छोटे आकार में विराट् को सहज पकड़ लेती है:
वृक्षवल्ली हमारे सगे वनचर
पक्षी भी गाते हैं सुस्वर.
ऐसे सुख से रुचता है एकान्त में वास
न आएं गुण-दोष हमारे पास.
आकाश मण्डप पृथ्वी आसन
क्रीड़ा करें जहां रमे मन.
कंथा, कमंडल काफ़ी है देह के लिए
समय का पता हमें वायु बतलाए
हरिकथा भोजन, अनेक व्यंजन
रुचि से सेवें, जो चाहे मन.
तुका कहे, होता है संवाद मन के साथ
अपनी ही अपने संग बात.
तुकाराम अपने बिम्ब अपने आसपास से चुनते हैं और उनमें फिर नयी अर्थाभा ले आते हैं: आस्था लगभग कौशल बन जाती है:
खटमल के लिए खटिया पर्वत
चढ़ना-उतरना कितना सारा.
वैसा था भाव अंदर
यह समझ में आया है.
बेर में बैठी इल्ली
उसकी दुनिया गुठली.
बीनकर खाता है चने
कहता है राजा हूं मैं
मेंढक कीचड़ खाये
क्या जान पाए, क्या है सागर
तुका कहे वैसा ही यहां है
भीतर क्या है, देखो.
तुकाराम प्रचलित धर्माचरण और अनुष्ठानों का प्रश्नांकन करते हुए कहते हैं: ‘मंदिर में देव, देव में मंदिर/खोजो तो मूल कहां है./मूल देखो तो, हम ही हैं मूल/ऐसी है गवाही अनुभव की,/नहीं मूल शाख, नहीं, जातिकुल/जो है अचल, रहे सदैव. देव न मंदिर, नहीं देवस्थान/काल और अकाल, नहीं वहां./भाव न भक्ति, मोक्ष न मुक्ति/दिन रात बीत गए…’ तुकाराम में बिम्बमयता है और अमूर्तन भी: ‘निरंजन में हमने बनाया घर, निराकार निरंतर/रहे हम. निराभास में पूर्ण/हुए समरस/अखण्ड एकत्व/ पाया हमने.’
मण्डला में
सर्वत्र पुण्या कही जानेवाली नर्मदा नदी मण्डला का मुख्य आकर्षण है. जिला मुख्यालय है पर अभी तक रेल वहां नहीं पहुंच पाई है. वहां चित्रकार रज़ा के पार्थिव अवशेष दफ़्न हैं ओर अब उनके नाम पर एक कलादीर्घा और सड़क हैं. रज़ा की मृत्यु को इसी 23 जुलाई को नौ बरस हो जाएंगे. इस बीच मण्डला ने अपने इस महान सपूत को धीरे-धीरे पहचानना शुरू किया है.
कुछ बच्चे, युवा और स्त्रियां पहचान रहे हैं. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वे ‘रज़ा स्मृति’ के अंतगर्त आयोजित कार्यशालाओं में स्क्रैप से मूर्ति बनाना, माटी और छातों को रंगना, गोंड़ चित्रांकन करना आदि सीखकर. अन्य नागरिक हिंदी के लगभग बीस कवियों का कविता-पाठ और ‘कविता का अरण्य’ विषय पर एक बातचीत सुनेंगे.
उन्हें रज़ा की अंतिम पूर्ण कलाकृति ‘स्वस्ति’ पर आधारित भरत नाट्यम और ओड़िसी की जुगलबन्दी और ‘राम की शक्तिपूजा’ नाट्य देखने का अवसर भी मिलेगा. कुल पांच दिनों में इतना कुछ रज़ा की मंगलछाया में. शायद ही देश में कहीं और ऐसे किसी चित्रकार को उद्बुद्ध किया जाता हो.
(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)